कविता को अपनी साँस कहने वाले
ये कवि मात्र एक कवि ही नहीं, एक उत्कृष्ट तेलुगु लेखक, समालोचक, अनुवादक, शिक्षा-शास्त्री और प्रशासक के साथ-साथ सुर, ताल, लय की अपार जानकारी रखने
वाले एक दक्ष गायक भी थे। अपने लिखे गीतों को जब वे मधुर स्वर-ताल में गा कर सुनाते
तो जनता मुग्ध हो कहती, "सिनारे! सिनारे!" ये लोकप्रिय गीतकार
जब साहित्यिक विद्वता में डूबते, तो उनकी कलम अठ्ठारह शैलियों में अद्भुत तेलुगु साहित्य
रच जाती। जब शिक्षण, आयोजन, प्रशासन का समय होता तो यही साहित्यिक हस्ताक्षर एक समय
के पाबंद, कम शब्दों में मन की बात कहने वाले, जल्दी निर्णय लेने वाले लोकप्रिय शिक्षक-प्रशासक
बन जाते। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, तेलुगु साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान डॉ० सी नारायण रेड्डी का पूरा नाम डॉ० सिंगिरेड्डी नारायण रेड्डी था। चिंगिरेड्डी
को तेलुगु में सिंगिरेड्डी बोला जाता है और इसीलिए
उनका छोटा नाम 'सिनारे' भी है। सिनारे तेलुगु के अत्यंत लोकप्रिय लेखक और विद्वान थे।
उनकी लिखी लंबी कविताओं, मुक्त-छंदों, गद्य-नाटकों, गीति-नाटकों, निबंधों,
साहित्यिक आलोचनाओं, अनुवादों और ग़ज़लों की लगभग ८५ प्रकाशित
पुस्तकों में उनकी लेखकीय विरासत दर्ज है। जहाँ एक ओर उनको मिले सम्मान- पद्मश्री,
पद्मभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और साहित्य अकादमी की फेलोशिप 'महत्तर सदस्यता' सिनारे के साहित्यिक अवदान के परिचायक हैं, वहीं दूसरी ओर तेलुगु
समाज में उनके फिल्मी गीतों पर मर मिटने वाले हज़ारों लोग उनकी लोकप्रियता और सहजता
का परचम फहराते हैं।
प्रारंभिक जीवन - कर्मभूमि
सिनारे आजीवन 'मनसा,
वाचा और कर्मणा' मानव के उत्थान पर केंद्रित रहे। "कविता मेरी मातृभाषा
है, उसका इतिवृत्त है मानवता" का
उद्घोष करने वाले इस महान लेखक का जन्म २९ जुलाई १९३१ को तेलंगाना के जनपद करीमनगर
के एक छोटे से गाँव हनुमाजीपेट में श्रीमती बुचाम्मा और श्री मल्ला रेड्डी के घर हुआ।
उनके माता-पिता किसान थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया।
नारायण ने करीमनगर से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई की लगन ऐसी कि आगे उन्होंने
हैदराबाद जा कर उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए किया। यह डिग्री उन्होंने उर्दू मीडियम
से हासिल की थी। उनके काव्य में इस का प्रभाव हम जल्दी ही देखेंगे।
उस्मानिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने १९५४ में एम० ए० (तेलुगु) की शिक्षा पूरी की और १९५५ में तेलुगु के व्याख्याता हुए।
अध्यापन के साथ-साथ उन्होंने अध्ययन जारी रखा और १९६२ में पीएचडी
कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग में अध्यापन किया। शिक्षाविद के
रूप में वे अत्यंत लोकप्रिय रहे और १९७६ में उस्मानिया में प्रोफ़ेसर बने। मधुर स्वर
में तेलुगु साहित्य पर दिए गए उनके व्याख्यानों की लोकप्रियता का यह आलम था कि अन्य
विभागों के छात्र अनुमति ले कर उनकी कक्षा में आ जाते और पूरा-पूरा व्याख्यान चुपचाप
बैठ कर सुनते। अध्यापन के क्षेत्र में आगे चल कर वे तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति
बने। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि सिनारे स्कूलों में भी तेलुगु को प्रथम भाषा
की तरह प्रतिष्ठित करने में सहायक थे, वरना विद्यार्थी कम अंकों के डर से तेलुगु लेना
पसंद नहीं करते थे।
नारायण की शादी सुशीला जी से हुई और उनकी चार पुत्रियाँ हुईं। उन्होंने अपनी पुत्रियों के नाम भारत की पवित्र नदियों
के नाम पर रखे - गंगा, यमुना, सरस्वती, और कृष्णवेणी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद
उनके नाम पर उन्होंने एक अवार्ड की स्थापना की, जिसे हर साल किसी प्रतिभाशाली महिला
लेखिका को दिया जाता है।
रचना
संसार
डॉक्टर श्रीनारायण रेड्डी का लेखन
बहुत उर्वर और विस्तृत रहा। "कविता मेरा पता है" शीर्षक से किताब
लिखने वाले इस विद्वान के हृदय की विश्रामस्थली वस्तुतः कविता ही थी। उनकी शुरुआती
शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई थी, इसीलिए उर्दू शायरी की रवायत
में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। तेलुगु के साथ-साथ उन्हें उर्दू, फ़ारसी,
अँग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं में भी महारत हासिल थी। ग़ज़ल लेखन में
वे तेलुगु और उर्दू, दोनों ही भाषाओं में सिद्धहस्त थे। उनकी
तेलुगू रचनाओं में उर्दू शायरी का सूक्ष्म प्रभाव मुक्त रूप से साँस लेता है। तेलुगु
भाषा पर उनका अद्वितीय अधिकार था। भाषा उनके
भावों के अनुरूप, उनकी लेखनी से निसृत होकर काव्य में ढल जाती।
१९५१ के आसपास इनकी सृजनशीलता
की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उस्मानिया विश्वविद्यालय में युवा स्नातक
छात्र के रूप में उन्होंने तेलुगु विभाग द्वारा आयोजित एक कवि सम्मेलन में भाग लिया।
इस सम्मेलन में उनकी आंदोलित करती कविताओं के कारण उनकी बड़ी वाह-वाही हुई। १९५२ में
जब वे मात्र बीस वर्ष के थे तब उनका पहला काव्य संकलन 'नव्वनि पुव्वु' (फूल जो नहीं
हँसा) प्रकाशित हुआ।
१९५९ में प्रकाशित 'वेन्नेल वाड' (चाँदनी भरा क़स्बा) उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है- यह रोमानी
संगीत-नाटकों की एक पुस्तक है जिसने तेलुगु लोकगीतों को आम पाठकों तक पहुँचाया। १९६४
में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक 'ऋतु चक्रम' आई। तेलुगु साहित्य-संसार
डॉ० रेड्डी जी को एक प्रयोगशील कवि मानता है। छह-सात दशक के निरंतर
काव्य सृजन के बावजूद डॉ० रेड्डी की कविताओं में एक ताज़गी सी
है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छंदयुक्त ही लिखा है, परंतु उनके मुक्त छंद में भी एक
गेयता है, एक लय है। उनकी लेखन शैली किसी अन्य लेखक से उधार नहीं ली गई, न ही उनकी
कविताएँ काल या कला से प्रतिबंधित हैं। उनकी कविताएँ तो मानवमूल्यों, आशा और मानवता
का जयघोष हैं। उनकी शुरुआती कविता में छायावाद और प्रयोगशीलता, दोनों के लक्षण मिलते
हैं। उनकी रचनाएँ निजी भाव, वृहद् मानव प्रेम, राष्ट्रीयता, आँचलिकता- इन सब का ऐसा
संयोजन हैं कि उनको किसी एक श्रेणी में रखना संभव नहीं। विश्व मानवता पर विश्वास रखने वाला यह कवि अपनी
किताब 'अक्षरों के गवाक्ष' में कहता है कि जब तक चिंतन की चिंगारी मानव मन में जलती
रहेगी, तब तक जीवन का ऊषा काल ही है, संध्या नहीं।
उनकी महत्त्वपूर्ण काव्य पुस्तक 'विश्वम्भरा' उन किताबों में से एक है जिसे एक ही साल में तीन महत्त्वपूर्ण पुरस्कार मिले। विश्वम्भरा वाचन काव्य परंपरा में लिखी गई पुस्तक है। पूरी सृष्टि के कैनवास पर लिखी यह एक अद्भुत और महत्त्वपूर्ण काव्यकृति है। विश्वम्भरा का तीन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ ने विश्वम्भरा के बारे में लिखा - "...अंततः अपनी महाकाव्य कविता विश्वम्भरा (१९८०) में मनुष्य की एक सार्वभौमिक दृष्टि के साथ उभरा। विश्वम्भरा उनकी महान कृति है जिसमें उन्होंने न केवल मुक्त छंद में महाकाव्य के एक नए रूप को विकसित किया, बल्कि कलात्मक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक उन्नति और आध्यात्मिक प्राप्ति की युगों से कोशिश कर रहे मनुष्य को अपनी त्रिकोणीय यात्रा में भी पेश किया। उनके सभी लेखन में गेय रोमांटिकवाद, आशावादी मानवतावाद, प्रगतिशील आदर्शवाद और स्वस्थ यथार्थवाद का एक अच्छा मिश्रण है।"
हिंदी में इसका अवुवाद डॉ० भीमसेन निर्मल (रीडर हिंदी विभाग, उस्मानिया विश्विद्यालय) ने किया है। इसका प्रथम हिंदी संस्करण १९८४ में लोकभारती प्रकाशन से आया था। 'विश्वम्भरा' एक प्रयोगशील, प्रतीक प्रधान काव्य है। यह मानव के उद्भव से मानव जीवन के विकास तक की यात्रा को दर्ज़ करती है। अनुवादक कहते हैं, "एक कुशल चित्रकार की तरह कवि ने इसमें अनेकानेक शब्द-चित्र प्रस्तुत किए, जिनका अनुवाद आसान नहीं था।" एक बानगी देखिए,
"ऋषिता
का, पशुता का
संस्कृति
का, दुष्कृति का
स्वच्छंदता
का, निर्बन्धता का
समार्द्रता
का, रौद्रता का
पहला
बीज है मन।
मन का
आवरण मानव
मानव
का आच्छादन जगत
यही है
विश्वम्भरा तत्व
यही है अनंत जीवन सत्य।"
विश्वम्भरा के लोकार्पण पर भव्य समारोह संपन्न हुआ जिसमें उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री एन० टी० रामाराव ने इसका विमोचन किया और पहली बार हिंदी में भाषण दिया। डॉ० रेड्डी अपनी कविताओं को सुमधुर ढंग से सुना कर श्रोताओं को बाँधने में माहिर थे ही, उस पर रामाराव जी के गंभीर मधुर स्वर - सोने पर सुहागा थे। सभा का आनंदोल्लास अवर्णनीय था। १९६८ से १९८२ तक के उनके साहित्यिक अवदान पर उन्हें १९८८ में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्हें पुरस्कार देते समय ज्ञानपीठ के पत्र में लिखा था, "डॉ० रेड्डी के अंदर एक रचनाकार की प्रतिभा और एक संचारक के आकर्षण का अद्भुत संयोजन है।"
डॉ० रेड्डी की ८० पृष्ठों की लंबी कविता 'भूमिका' का अनुवाद
उस्मानिया विश्विद्यालय की प्रोफेसर माणिक्याम्बा मणि ने किया।
काव्य के अतिरिक्त सिनारे ने तेलुगु में स्वयं कई महत्वपूर्ण अनुवाद किए और शोध प्रबंध भी लिखे। मीरा, गाँधी, खलील जिब्रान आदि के
अमर कृतियों/कथनों का उन्होंने अनुवाद किया है। १९६७ में लिखा उनका शोध प्रबंध 'आधुनिक आंध्र कविता : परंपरा एवं प्रयोग' साहित्यिक तबकों
में बहुचर्चित रहा।
सिनारे ने केवल गंभीर साहित्य
ही नहीं बल्कि ३५०० से अधिक फ़िल्मी गीत भी लिखे। १९६२ में एन० टी० रामाराव ने फ़िल्म 'गुलेबकावली कथा' में पहली बार उनसे सारे गीत लिखवाए,
जिसमें सुपरहिट गीत 'नन्नु दोचु कुंदुवटे' भी शामिल है। सिनारे भाषा-सौंदर्य से भरे गीत लिखने के लिए प्रतिबद्ध रहे और फ़िल्मी कामयाबी या ग़ैर-कामयाबी
की चिंता और दवाब भी उन्हें भाषा की शुद्धता से डिगा न सके। उन्होंने जनपदीय भाषा (बोली) में संदर्भ के अनुरूप
फिल्मों के लिए श्रुतिमधुर गीतों की रचना भी की जो लोकगीत की
परंपरा के वाहक बने। १९६५ में डॉक्टर रेड्डी महासचिव के रूप में प्रपंच (विश्व) तेलुगु
लेखक सम्मेलन के वार्षिक समारोह के आयोजन में सहायक रहे और उन्होंने आयोजन में महत्वपूर्ण
योगदान दिया।
लेखन के लिए १९७७ में उन्हें पद्मश्री और १९९२ में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। डॉ० रेड्डी को अगस्त १९९७ में राजयसभा के लिए मनोनीत किया गया। वे एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए राजनीति की तंग गलियों में भी हर मोड़ पर उनके दोस्त थे। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में भी अपने काम से अपनी पहचान बनाई। राज्यसभा में उनके दिए गए भाषणों पर २०१९ में एक किताब भी निकली है। उनके परम मित्र न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर अपनी ४५ वर्ष की दोस्ती को याद करते हुए कहते हैं, "इंदिरा पार्क में सुबह की सैर करते हुए नारायण की कविताओं का पहला श्रोता मैं था।"
नारायण रेड्डी तेलुगू भाषा और
साहित्य में महारत रखने वाले शब्द-साधक ही नहीं शब्द-शासक भी थे। साहित्य सभाओं में अपनी प्रवाहमयी वाग्मिता से वे तेलुगु
भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और तेलुगु को युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने
के प्रति समर्पित थे।
१२ जून २०१७ को ८५ वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में उनकी साँसों की कविता ने उनसे विदा ली और उनका निधन हो गया। यह तेलुगु ही नहीं, भारतीय साहित्य की भी गहरी क्षति थी। उनके निधन पर गवर्नर सी० विद्यासागर राव ने कहा, "डॉक्टर रेड्डी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तेलंगाना के अतिविशिष्ट कवियों और लेखकों में सर्वोत्तम थे। उनके जाने से तेलुगु का एक सितारा खो गया है। यह क्षति कोई भी पूरी नहीं कर सकेगा।"
कविता को साँसों में बसाने वाले की अपनी ही साँसें रुक जाएँ तो काव्य संसार में एक अभेद्य मौन छा जाता है, यह मौन उनके प्रशंसकों को आज भी महसूस होता है।

चित्र १ : सी० नारायण रेड्डी जी की लंबी कविता की किताब 'भूमिका' के मणि जी द्वारा किए हिंदी अनुवाद की पुस्तक का लोकार्पण समारोह। यहाँ चित्र में रेड्डी जी, मणि जी के साथ हैं, वाइस चांसलर प्रो० अभय मौर्या।

चित्र २ : प्रो० मणि श्री नारायण रेड्डी से एन० गोपी की रचना "जलगीत" के अनुवाद पर प्रशस्ति लेते हुए।
|
सी० नारायण रेड्डी |
|
|
नाम |
डॉ० चिंगिरेड्डी/सिंगीरेड्डी नारायण रेड्डी 'सिनारे' |
|
जन्म |
२९ जुलाई १९३१ (करीम, हनुमाजीपेत, तेलंगाना) |
|
माता / पिता |
श्रीमती बुचाम्मा और श्री मल्ला रेड्डी |
|
प्राथमिक शिक्षा |
करीमनगर से हाई स्कूल पास |
|
उच्च शिक्षा |
बीए व एमए (तेलुगु) उस्मानिया
विश्वविद्यालय हैदराबाद, १९५४ पीएचडी, १९६२ |
|
कार्यक्षेत्र |
प्रोफ़ेसर, कुलपति, राजयसभा सदस्य, कवि,
लेखक, आलोचक, आयोजक, सिनेगीत लेखक |
|
मुख्य किताबें |
|
|
गेय काव्य |
फूलों के गीत (१९५१-५२) |
|
गेय नाटक |
अनहँसा फूल (१९५३), अजंता सुंदरी (१९५५),
ज्योत्स्ना वीथी (१९५९), पीढ़ियों की तेलुगु ज्योति (१९७५) |
|
खंड काव्य |
जल प्रपात (१९५३), नारायण रेड्डी के गीत
(१९५५), दीपों के नूपुर (१९५९), अक्षरों के गवाक्ष (१९६५), मध्यवर्ग का मंदहास (१९६८),
एक और इंद्रधनुष (१९६९), आग और इंसान(१९७०), आमने-सामने (१९७१), इंसान और तोता (१९७२),
उदय है मेरा हृदय (१९७३), परिवर्तन है मेरा फैसला (१९७४), तेज है मेरी तपस्या (१९७५),
घर का नाम है चैतन्य (१९७६), मंथन(१९७८), मृत्यु से (१९७९), विश्वम्भरा
(१९८१) |
|
सुदीर्घ गीति-काव्य
|
विश्वगीति (१९५४), भूमिका (१९७७) |
|
इतिवृत्तात्मक गेय-काव्य |
नागार्जुन सागर (१९५५), स्वप्न भांग (१९५७)
कर्पूर वसंतराय (१९५७), विश्वनाथ नायक (१९५९), ऋतुचक्र (१९६४), निखरा राष्ट्र का
रत्न पंडित नेहरू (१९६७) |
|
गीति-नाटक |
रामप्पा का मंदिर (१९६०), नारायण रेड्डी की
नाटिकाएँ (१९७८) |
|
गेय सूक्ति संकलन |
समदर्शन (१९६०) |
|
निबंध संकलन |
व्यास वाहिनी (१९६५), हमारा गाँव बोल उठा
(१९८०), समीक्षणं (१९८१) |
|
शोध प्रबंध |
आधुनिक आंध्र कविता : परंपरा एवं प्रयोग (१९६७) |
|
अनुवाद |
गाँधीयम (१९६९) - महात्मा गाँधी जी की सूक्तियों
का अनुवाद मीराबाई (१९७२) - मीरा के ५० पदों का अनुवाद
चोटियाँ और घाटियाँ (१९७४) - खलील जिब्रान का
अनुवाद मोतियों की कोयलिया (१९७९) - सरोजिनी नायडू
के ५० गीतों का अनुवाद |
|
व्याख्या |
मंदार मकरंद (भक्त प्रवर पोतन्ना के ५० पद्यों
की व्याख्या |
|
यात्रा संस्मरण |
शौक के तीन सप्ताह (यूरोप की यात्रा) सोवियत रूस में दस दिन पाश्चात्य देशों में पचास दिन फिर रूस में |
|
सिनेगीत |
तीन हज़ार पाँच सौ से अधिक सिनेमा गीत। एक
संकलन - दिन में ही खिली चाँदनी |
|
मुख्य सम्मान |
साहित्य अकादमी पुरस्कार, १९७३ पद्मश्री, १९७७ कला प्रपूर्ण १९७८ महाकवि कुमारन आसान पुरस्कार (केरल) भीलवाड़ा पुरस्कार (कोलकोता) सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार ज्ञानपीठ, १९८८ पद्मभूषण, १९९२ साहित्य अकादमी की फेलोशिप 'महत्तर सदस्यता',
२०१५ |
संदर्भ
- साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्य्ता पत्र
- विश्वम्भरा पुस्तक
- https://en.wikipedia.org/wiki/C._Narayana_Reddy#
- https://www.jstor.org/stable/26791499
- Veteran Telugu poet, writer C Narayana Reddy passes away
- https://www.loc.gov/acq/ovop/delhi/salrp/reddy.html
लेखक परिचय






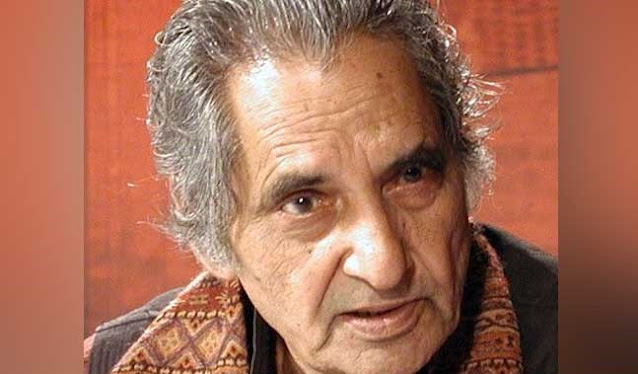
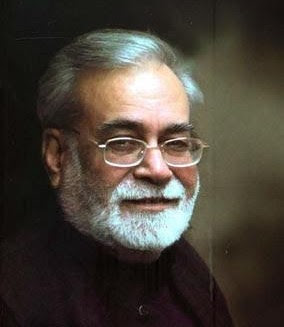











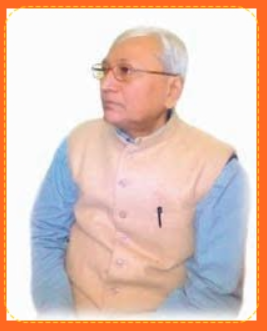

ReplyDeleteतेलुगु साहित्य के विद्वान् नारायण रेड्डी पर बहुत सुंदर, शोध परक, ज्ञानवर्धक, दिलचस्प और प्रशंसनीय आलेख के लिए मणिजी और शार्दुला हार्दिक बधाई स्वीकार करें l तेलुगु साहित्य आकाश के जगमगाते सितारे नारायण रेड्डी को आपने हिंदी पाठकों तक पहुँचाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। इसके लिए धन्यवाद आप दोनों को।
कविता को अपनी साँस, मातृभाषा और पता बताने वाले इस महान शब्द-साधक से परिचय कराने के लिए आदरणीय मणि जी व शार्दूला जी का बहुत आभार। बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया आपने। मन पर कविता पढ़कर उन्हें और पढ़ने का मन हो आया है।
ReplyDeleteअद्भुत! तेलगु भाषा की कविता की आत्मा ‘सिनारे’ जी का परिचय मन को भा गया। आलेख का प्रवाह और रूह दोनों क़ाबिले तारीफ़ हैं। आलेख में मणि जी की उपलब्धियों की झलक भी दिखी। उनके लिए मणि जी को तहे दिल से बधाई। लेखिका द्वय, मणि जी और शार्दुला को इस आलेख के लिए अनेकानेक बधाइयाँ। ग़ैर-हिंदी भाषी साहित्यकारों को जानकर हम निश्चित रूप से समृद्ध हो रहे हैं। इस अनुपम काम के लिए जुड़े सभी लोगों का आभार।
ReplyDeleteमणि जी एवं शार्दुला जी नमस्ते। आप दोनों को इस बेहतरीन लेख के लिए हार्दिक बधाई। आप के द्वारा प्रस्तुत आज के लेख की जितनी प्रसंशा की जाए कम है। पढ़कर आंनद आया। इस लेख के माध्यम से डॉ. सी नारायण रेड्डी जी के साहित्यिक योगदान को विस्तार से जानने का अच्छा अवसर मिला।
ReplyDeleteमेहनत से किया गया शोध, उमंग में लिखी गई भाषा और तरतीब से नियोजित प्रस्तुति , यह मिलकर ऐसा आलेख बनाते हैं । मणि जी, शार्दुला जी, आपने सिनारे से ऐसे परिचय कराया कि लगता है, उन्हें बरसों से जानते हैं। विश्वंभरा तो अब पढ़नी ही होगी। आप दोनों को बधाई।सदैव ऐसे ही लिखते रहने के लिए शुभकामना !💐💐
ReplyDeleteकविता को अपनी सांस बताने वाले महान साहित्यकार सिनारे जी पर सरल,सहज व सुंदर शब्दों में मणि जी और शार्दुला जी की ये प्रस्तुति अभिनंदनीय है..
ReplyDeleteममता किरण