
पं० विद्यानिवास मिश्र का जन्म २८ जनवरी १९२६ को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर ज़िले के पकडडीहा गाँव में हुआ था।वाराणसी और गोरखपुर में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्री मिश्र ने सन १९४५ में 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय' से स्नातकोत्तर की उपाधि और गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष १९६०-६१ में पाणिनी की व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। डॉ० विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जाने-माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार और नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ललित निबंध परंपरा में इन्हें आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ त्रिमूर्ति का तीसरा स्तंभ कहा गया है। पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई हिंदी साहित्यकार ललित निबंधों को वांछित ऊँचाइयों पर ले गया, तो डॉ० विद्यानिवास मिश्र का ही नाम लिया जाता है। आपकी विद्वता से हिंदी जगत का कोना-कोना परिचित है। कुछ समय के लिए आप अमेरिका गए, वहाँ कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्यापन किया एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भी हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। उन्होंने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया और वर्ष १९६७-६८ में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में ही अध्येता के रूप में कार्यरत रहे। लगभग दस वर्षों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो, विंध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में नौकरी के बाद आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। वे १९६८ से १९७७ तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। कुछ वर्षों के बाद वे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आपने 'वाणरासेय संस्कृत विश्वविद्यालय' में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। राष्ट्रहित में आपकी साहित्यिक सफलताओं को तरजीह देते हुए, भारत सरकार द्वारा सांसद के रूप में भी नियुक्त किया गया। प्रो० मिश्र 'भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य और मूर्ति देवी पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे। प्रो० विद्यानिवास मिश्र स्वयं को 'भ्रमरानंद' कहते थे और इस छद्मनाम से आपने बहुत अधिक लिखा है। आप हिंदी के एक प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंध लेखक हैं; साहित्य की इन दोनों ही विधाओं में आपका कोई विकल्प नहीं हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों की शृंखला काफी लंबी है। उन्हें अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति के कारण हर मोर्चे पर हमेशा सराहा गया।
साहित्यिक उपलब्धियाँ
साहित्यिक उपलब्धियाँ
प्रो० विद्यानिवास मिश्र ने हिंदी जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। ललित निबंध विधा की शुरुआत के रूप में उनका पहला निबंध संग्रह १९५२ ईसवी में 'चितवन की छाँह' शीर्षक से पाठकों के समक्ष आया। श्री मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने-माने भाषाविद थे। हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन की सुगंध से सुवासित करने वाले विद्यानिवास मिश्र ऐसे साहित्यकार थे, जिन्होंने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच के साथ खपाने का दुरूह प्रयास किया। साहित्य-समीक्षकों और समालोचकों के अनुसार संस्कृत मर्मज्ञ श्री मिश्र ने हिंदी में सदैव आँचलिक बोलियों, विशेष रूप से भोजपुरी के शब्दों को भरपूर महत्त्व दिया। डॉ० विद्यानिवास मिश्र के अनुसार - "हिंदी में यदि आँचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए, तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद संस्कृतनिष्ठ है।"
श्री मिश्र की ७० से अधिक प्रकाशित कृतियाँ हैं, जिनमें व्यक्तिव्यंजक निबंध-संग्रह, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक कृतियाँ, भाषा चिंतन के क्षेत्र में शोध ग्रंथ और कविता-संकलन सम्मिलित हैं। डॉ० विद्यानिवास मिश्र आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, सामाजिक संस्कृति, साहित्य कला की नवीनतम चेतना और तेज से मंडित साहित्य पुरोधा हैं। श्री विद्यानिवास मिश्र की हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा में भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें "महाभारत का कव्यार्थ" और "भारतीय भाषादर्शन की पीठिका" प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ललित निबंधों में "तुम चंदन हम पानी", १९५२, "वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं", १९७२ बहुत ही चर्चित कृतियाँ हैं। अन्य ग्रंथों में निम्नलिखित शामिल हैं :- स्वरूप-विमर्श, २००१ (सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध निबंधों का संकलन), कितने मोरचे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आरपार, अग्निरथ, लागो रंग हरो, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दें (घुसपैठियों पर आधारित निबंध), फागुन दुइ रे दिना, १९९४, भारतीय संस्कृति के आधार, भ्रमरानंद का पचड़ा, रहिमन पानी राखिए (जल पर आधारित निबंध), राधा माधव रंग रंगी (गीतगोविंद की सरस व्याख्या), लोक और लोक का स्वर (लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति), वाचिक कविता अवधी (वाचिक अवधी कविताओं का संकलन), वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति-व्यंजना (विशिष्ट व्यक्त व्यंजक निबंध), सपने कहाँ गए (स्वाधीनता संग्राम पर आधारित पुस्तक), साहित्य के सरोकार, २००७, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, काव्य संग्रह - पानी की पुकार, आलोचनात्मक ग्रंथ - तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कबीर वचनामृत, रहीम रचनावली, रसखान ग्रंथावली आदि। इनके अतिरिक्त, इन्होंने अनेक समीक्षात्मकऔर शोधग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें 'हिंदी की शब्द संपदा', 'पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति', 'रीति विज्ञान' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
पुरस्कार एवं सम्मान
भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हें 'पद्मश्री'और 'पद्मभूषण' जैसी उपाधियों से सम्मानित किया।संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य के मर्मज्ञ डॉ० मिश्र को अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया और वे ऐसी संस्थाओं के आजीवन सदस्य भी रहे। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए - पद्मश्री -१९८८, मूर्ति देवी पुरस्कार (ज्ञानपीठ) – १९८९, विश्व भारती सम्मान-१९९६, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सम्मान - १९९६, पद्मभूषण - १९९९, मंगलाप्रसाद पारितोषिक - २००१, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, के०के०बिड़ला फाउंडेशन के चौथी श्रेणी का सम्मान-शंकर सम्मान आदि।
साहित्यिक विशेषताएँ
पं० विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में संस्कृति एवं लोक तत्व तो समाविष्ट है। इसके अलावा उनके निबंधों में विचार, अनुभूति, बुद्धि, कल्पना, कला एवं शैली का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। व्यक्तिव्यंजक और ललित निबंधकारों में पं० विद्यानिवास मिश्र का स्थान अग्रणी है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ-साथ भावुकता उनके निबंधों में जगह-जगह झलकती दिख जाती है। एक ललित निबंधकार के रूप में मिश्रजी ने हिंदी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।साथ ही, मिश्र जी के ललित निबंधों में भावात्मकता और लोक संस्कृति की छटा भी विद्यमान है। इनके निबंधों में प्रसादमयी भाषा-शैली, कथात्मक चित्रों की अधिकता और विवेचना की तथ्यपूर्ण गंभीरता दिखाई देती है। अज्ञेय के अनुसार,
श्री मिश्र की ७० से अधिक प्रकाशित कृतियाँ हैं, जिनमें व्यक्तिव्यंजक निबंध-संग्रह, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक कृतियाँ, भाषा चिंतन के क्षेत्र में शोध ग्रंथ और कविता-संकलन सम्मिलित हैं। डॉ० विद्यानिवास मिश्र आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, सामाजिक संस्कृति, साहित्य कला की नवीनतम चेतना और तेज से मंडित साहित्य पुरोधा हैं। श्री विद्यानिवास मिश्र की हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा में भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें "महाभारत का कव्यार्थ" और "भारतीय भाषादर्शन की पीठिका" प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ललित निबंधों में "तुम चंदन हम पानी", १९५२, "वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं", १९७२ बहुत ही चर्चित कृतियाँ हैं। अन्य ग्रंथों में निम्नलिखित शामिल हैं :- स्वरूप-विमर्श, २००१ (सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध निबंधों का संकलन), कितने मोरचे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आरपार, अग्निरथ, लागो रंग हरो, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दें (घुसपैठियों पर आधारित निबंध), फागुन दुइ रे दिना, १९९४, भारतीय संस्कृति के आधार, भ्रमरानंद का पचड़ा, रहिमन पानी राखिए (जल पर आधारित निबंध), राधा माधव रंग रंगी (गीतगोविंद की सरस व्याख्या), लोक और लोक का स्वर (लोक की भारतीय जीवनसम्मत परिभाषा और उसकी अभिव्यक्ति), वाचिक कविता अवधी (वाचिक अवधी कविताओं का संकलन), वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति-व्यंजना (विशिष्ट व्यक्त व्यंजक निबंध), सपने कहाँ गए (स्वाधीनता संग्राम पर आधारित पुस्तक), साहित्य के सरोकार, २००७, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, काव्य संग्रह - पानी की पुकार, आलोचनात्मक ग्रंथ - तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कबीर वचनामृत, रहीम रचनावली, रसखान ग्रंथावली आदि। इनके अतिरिक्त, इन्होंने अनेक समीक्षात्मकऔर शोधग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें 'हिंदी की शब्द संपदा', 'पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति', 'रीति विज्ञान' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
पुरस्कार एवं सम्मान
भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हें 'पद्मश्री'और 'पद्मभूषण' जैसी उपाधियों से सम्मानित किया।संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य के मर्मज्ञ डॉ० मिश्र को अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया और वे ऐसी संस्थाओं के आजीवन सदस्य भी रहे। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए - पद्मश्री -१९८८, मूर्ति देवी पुरस्कार (ज्ञानपीठ) – १९८९, विश्व भारती सम्मान-१९९६, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सम्मान - १९९६, पद्मभूषण - १९९९, मंगलाप्रसाद पारितोषिक - २००१, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, के०के०बिड़ला फाउंडेशन के चौथी श्रेणी का सम्मान-शंकर सम्मान आदि।
साहित्यिक विशेषताएँ
पं० विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में संस्कृति एवं लोक तत्व तो समाविष्ट है। इसके अलावा उनके निबंधों में विचार, अनुभूति, बुद्धि, कल्पना, कला एवं शैली का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। व्यक्तिव्यंजक और ललित निबंधकारों में पं० विद्यानिवास मिश्र का स्थान अग्रणी है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ-साथ भावुकता उनके निबंधों में जगह-जगह झलकती दिख जाती है। एक ललित निबंधकार के रूप में मिश्रजी ने हिंदी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।साथ ही, मिश्र जी के ललित निबंधों में भावात्मकता और लोक संस्कृति की छटा भी विद्यमान है। इनके निबंधों में प्रसादमयी भाषा-शैली, कथात्मक चित्रों की अधिकता और विवेचना की तथ्यपूर्ण गंभीरता दिखाई देती है। अज्ञेय के अनुसार,
''विद्यानिवास जी ने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चखा है और लोकवाणी की गौरव गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ललित निबंध वह लिखते हैं, तो लालित्य के किसी मोह से नहीं, इसलिए कि गहरी, तीखी, चुनौती भरी बात भी एक बेलाग और निर्दोष बल्कि कौतुकभरी सहजता से कह जाते हैं।''
मिश्रजी के निबंधों को विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक एवं संस्मरणात्मक - इन पांच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, किंतु उसमें उर्दू, अंग्रेज़ी एवं ग्रामीण जीवन में रचे-बसे लोकभाषा के शब्द भी खूब मिलते हैं। शैली की विविधता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। आलंकारिक शैली, तरंग शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली उनके निबंधों में देखने को मिलती है। मिश्र जी के निबंधों में लोकजीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठा है। किसी भी प्रसंग को लेकर वे उसे ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक संदर्भों से युक्त कर लोकजीवन से जोड़ देने की कला में पारंगत हैं। उनके निबंधों में लोकतत्व का भरपूर समावेश है। विशेष रूप से भोजपुरी लोकजीवन उनके निबंध में गहरे से समाया हुआ है। मिश्र जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा कलात्मक संदर्भों से युक्त करके इतना प्रभावशाली बना देते हैं, जिससे उन्हें पढ़ते ही मन प्रसन्न हो जाता है और पाठक कहीं न कहीं खुद को कथानक से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मिश्र जी के ललित निबंधों में शास्त्र-संपदा, लोक-संस्कृति एवं कला चिंतन की भी झलक दिखाई देती है। मिश्र जी के ललित निबंध विषय-वस्तु, शैली-शिल्प एवं भाव-भंगिमा की दृष्टि से अभूतपूर्व हैं। मिश्र जी के निबंधों में केवल कल्पना की उडान नहीं, अपितु समसामयिक समस्याओं एवं जीवन की विषमताओं का निरूपण व्यंग्यपूर्ण शैली में किया गया है। अपनी सांस्कृतिक-चेतना के प्रति आपका सजग आक्रोश ही इन निबंधों में व्यक्त हुआ है और उन्हें पठनीय बना देता है। आपके निबंधों में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा तथा प्रेम दिखाई पड़ता है। उनके निबंधों में भारतीय परिवेश, संस्कृति तथा कला, समग्रता के साथ अभिव्यक्त हुई है। डॉ० विद्यानिवास मिश्र उच्च कोटि के कला चिंतक और समर्थ साधक जान पड़ते हैं और उनके निबंधों में उनका कला चिंतन भी यत्र-तत्र-सर्वत्र दिखाई पड़ता है।
'चितवन की छांह' निबंध संग्रह की भूमिका में अपनी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, वे कहते हैं कि अनजाने आदमी की अपनी अनजानी ग़लती के इतिहास को भी यदि कोई भूमिका कहना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भूमिका के स्वीकृत माने में यह भूमिका नहीं है। असल में लक्षणा की कृपा कहिए या अर्थ-विस्तार का जादू कि आज भूमिका का अर्थ है, भूमि को छोड़कर आकाश-पाताल एक करते हुए अंत में अंतरिक्ष में ओझल हो जाना, पर लोगों की नम्रता है कि उसे आकाशिका, पातालिका या अंतरिक्षिका न कहकर महज़ भूमिका कह देते हैं। सो मेरी वैसी क्षमता नहीं है, मैं तो अपने निबंध-लेखन की विशेषताओं का बयान करने जा रहा हूँ। उस बयान की यह लंबी-चौड़ी भूमिका ज़रूर मैंने बाँधी है, पर बयान मेरा सीधा सपाट होगा इतना विश्वास रखिए। संस्कृत के पठन-पाठन की ही मेरे कुल में परंपरा रही है, पर मैं रुद्री के ‘गणनां त्वां’ के आगे न जा सका और ए,बी ,सी ,डी सीखने लगा। विश्वविद्यालय में पहुँचते-पहुँचते संस्कृत अध्ययन की ओर मेरा प्रत्यावर्त्तन हुआ और तभी एक ओर राबर्ट लुई स्टीवेंसन, टामस डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम्ब और स्विफ्ट की कलमनवीसी से प्रभावित हुआ; दूसरी ओर बाणभट्ट, भवभूति एवं अभिनवगुप्त, पादाचार्य की भाषा शक्ति का भक्त बना। मेरी तबियत भी गुलेरी, पूर्णसिंह माधव मिश्र और बालमुकुंद गुप्त की डगर पर चलने के लिए मचलने लगी और काग़ज़-स्याही का मैंने काफ़ी दुरुपयोग भी किया। भाषा आडंबर के पचीसों ठाठ बाँधें और उधेड़ दिए। यहाँ तक कि उन दिनों मित्रों के पास पत्र भी लिखता तो पन्ने रंग देता, बहुत से दाद भी देते और बहुतेरे तो चमत्कृत होकर रह जाते, कुछ जवाब ही नहीं देते। बाद में कुछ दिनों के लिए यह रसीला व्यापार जब केवल एक गँवई वाली तक सीमित रह गया और उधर से प्रत्याशित प्रतिदान न मिलने से निराशा होने लगी, तब मेरी आँखें संस्कृत के समास से भोजपुरी के व्यास की ओर एकदम खिंच आईं। साहित्य का अधकचरा अध्ययन, मित्रों का प्रोत्साहन, पूरबी का स्नेहांचल विज़न और अपना बेकार जीवन...मेरे मध्य वित्तीय निबंधों को यही ध्यान मिला है। मैं पूर्वोक्त रससिद्ध लेखकों का ऋणी हूँ, यह कहकर उनको भी अपने साथ घसीटूँ, इतना दुस्साहस मुझमें नहीं है, किंतु जिन मित्रों ने मुझे इस ओर आने के लिए प्रोत्साहित क्यों दुरुत्साहित किया है, उनके नाम मैंने अपने आभार में गिना दिए हैं। व्यक्तियों के प्रभाव की बात तो यह हुई, जिन विचारों की छाप मेरे ऊपर मेरी जानकारी में पड़ी है, उनका भी कुछ ब्यौरा दे दूँ। व्यक्तिप्रधान निबंधों में कुछ लोग विचारत्व की ख़ास उपयोगिता नहीं देखते और वैसे लोगों को शायद मेरे निबंधों में विचारत्व दिखे भी न, परंतु मैं अपनी आस्थाओं का अभिनिवेश रखे बिना कहीं भी नहीं रहना चाहता, निबंध में तो और भी नहीं। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है, मैं रेती में अपनी डेंगी नहीं चलाना चाहता और न ज़मीन के ऊपर बने रुँधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। इसलिए प्रचलित शब्दावली में अगर प्रगतिशील नहीं हूँ, तो कम-से-कम प्रतिगामी भी नहीं ही हूँ। वैसे अगर भारत के राम और कृष्ण तथा सीता और राधा को प्रगति के दायरे से मतरूक़ न घोषित किया जाए, तो मैं भी अच्छा ख़ासा प्रगतिशील अपने को कह सकता हूँ, और अगर राम और कृष्ण के नाम के साथ प्रतिगामिता लगी हुई हो, तो मुझे प्रतिगामी कहलाने में सुख ही है। कुछ दिनों तक सम्मेलन की राजनैतिक गोलबन्दी में ज़रूर पड़ गया था, पर किसी साहित्यिक गोलबन्दी में मैं शरीक नहीं रहा हूँ। इसलिए न मुझको किसी का वरद हस्त प्राप्त है, न किसी के पूर्वग्रह का कड़वा घूँट ही। मानवता की समानभूमि पर मुझे सभी मिल जाते हैं। यों तो 'सहस नयन' 'सहस दस काना' और 'दो सहस' रसना वाले प्रणम्य महानुभाव जो न देख-सुन-कह सकें, उनसे मैं पनाह माँगता हूँ। इतना मैं और कह दूँ कि विलायती चीजों के आदान से मुझे विरोध नहीं है, बशर्ते उतनी मात्रा में प्रदान करने की अपने में क्षमता भी हो। इस सिलसिले में मुझे काशी के एक व्युत्पन्न पंडित के बारे में सुनी कहानी याद आ रही है। उन पंडित के पास जर्मनी से कुछ विद्वान आये (शायद उन दिनों जो विद्वान संस्कृत सीखने आते थे, उनका घर जर्मनी ही मान लिया जाता था, खैर) और उनके पास टिक गए। स्वागत-सत्कार करते-करते पंडित जी को एक दिन सूझ आई कि इन लोगों को भारतीय भोजन भारतीय ढंग से कराया जाए। सो वह इन्हें गंगा जी में नौका-विहार के लिए ले गए और गरमा-गरम कचालू बनवाकर भी लेते गए। नाव पर कचालू दोने में परोसा गया, पंडित जी ने भर मुँह-कौर कचालू झोंक लिया, इसलिए उनकी देखादेखी जर्मन साहबों ने भी काफ़ी कचालू एक साथ मुँह में डाला, और बस मुँह में जाने की देरी थी, लाल मिर्च का उनके संवेदनशील सुकंठ से संस्पर्श होते ही, वे नाच उठे और कोट-पैंट डाले ही एकदम गंगा जी में कूद पड़े। किसी तरह मल्लाहों ने उन्हें बचाया। पर इसके बाद उनका ‘अदर्शनं लोपः’ हो गया। दूसरे लोगों ने पंडित जी को ऐसी अभद्रता के लिए भलाबुरा कहा, तो उधर से जवाब मिला..."इन लोगों ने हमें अंडा-शराब जैसी महँगी और निशिद्ध चीजे़ं खानी सिखलाईं, तो ठीक और मैंने शुद्ध चटपटे भारतीय भोजन की दीक्षा एक दिन इन लोगों को देने की कोशिश की तो मैं अभद्र हो गया?", लोग इस उत्तर से निरुत्तर हो गए। तो कहने का मतलब यह कि आदान-प्रदान का यह भी एक तरीका है और शास्त्रसम्मत तरीका है, काशीधाम की इस पर मुहर लगी हुई है। परंतु मैं साहित्य में ऐसे आदान-प्रदान का पक्षपाती नहीं हूँ। सूफ़ियों और वेदांतियों के जैसे आदान-प्रदान का मैं स्वागत करने को तैयार हूँ, नहीं तो अपनी बपौती बची रहे, यही बहुत है। इस प्रसंग में आज नाम आता है, मार्क्स और फ्रायड का। अर्थ और काम के विवेचन में इनकी देन महनीय है, इसमें संदेह नहीं किंतु जब भारत में इनके अनुकूलन (एडाप्टेशन) की बात आती है, तो बरबस हमारा ध्यान अपने धर्म की ओर चला जाता है। 'रिलीजन' से 'धर्म' में कितना भेद है, यह जो नहीं जानता वह भारतीय संस्कृति की समन्विति का ठीक-ठीक साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। जन संस्कृति की बात भी जो लोग आज बहुत करते हैं, वे 'जन' का इतिहास परखे बिना ही। भारत का धर्म किसी शासन-व्यवस्था का कवच या आवरण नहीं है, वह स्वयं भारतीय जीवन का अंतर्मर्म है। उस धर्म के जितने लक्षण कहे गए हैं, सबमें से यही ध्वनि निकलती है "चोदना लक्षणो धर्मः", आगे बढ़ने की प्रेरणा धर्म है, "यतोऽभ्युदयनिः श्रेयः संसिद्धि स धर्मः" जिससे अभ्युदय और परम और विश्वव्यापी कल्याण हो, वह धर्म है। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों में समरसता स्थापित करने वाला माध्यम है। उस धर्म पर ऐंठन ज़रूर पड़ता गई, पर इन खोलों को चीरने के बजाय भारतीय जीवन के मूल को उखाड़ फेंकना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मार्क्स और फ्रायड की स्थापनाओं के शीर्ष पर व्यास का यह वाक्य मुझे झिलमिलाता मिलता है -
'चितवन की छांह' निबंध संग्रह की भूमिका में अपनी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, वे कहते हैं कि अनजाने आदमी की अपनी अनजानी ग़लती के इतिहास को भी यदि कोई भूमिका कहना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भूमिका के स्वीकृत माने में यह भूमिका नहीं है। असल में लक्षणा की कृपा कहिए या अर्थ-विस्तार का जादू कि आज भूमिका का अर्थ है, भूमि को छोड़कर आकाश-पाताल एक करते हुए अंत में अंतरिक्ष में ओझल हो जाना, पर लोगों की नम्रता है कि उसे आकाशिका, पातालिका या अंतरिक्षिका न कहकर महज़ भूमिका कह देते हैं। सो मेरी वैसी क्षमता नहीं है, मैं तो अपने निबंध-लेखन की विशेषताओं का बयान करने जा रहा हूँ। उस बयान की यह लंबी-चौड़ी भूमिका ज़रूर मैंने बाँधी है, पर बयान मेरा सीधा सपाट होगा इतना विश्वास रखिए। संस्कृत के पठन-पाठन की ही मेरे कुल में परंपरा रही है, पर मैं रुद्री के ‘गणनां त्वां’ के आगे न जा सका और ए,बी ,सी ,डी सीखने लगा। विश्वविद्यालय में पहुँचते-पहुँचते संस्कृत अध्ययन की ओर मेरा प्रत्यावर्त्तन हुआ और तभी एक ओर राबर्ट लुई स्टीवेंसन, टामस डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम्ब और स्विफ्ट की कलमनवीसी से प्रभावित हुआ; दूसरी ओर बाणभट्ट, भवभूति एवं अभिनवगुप्त, पादाचार्य की भाषा शक्ति का भक्त बना। मेरी तबियत भी गुलेरी, पूर्णसिंह माधव मिश्र और बालमुकुंद गुप्त की डगर पर चलने के लिए मचलने लगी और काग़ज़-स्याही का मैंने काफ़ी दुरुपयोग भी किया। भाषा आडंबर के पचीसों ठाठ बाँधें और उधेड़ दिए। यहाँ तक कि उन दिनों मित्रों के पास पत्र भी लिखता तो पन्ने रंग देता, बहुत से दाद भी देते और बहुतेरे तो चमत्कृत होकर रह जाते, कुछ जवाब ही नहीं देते। बाद में कुछ दिनों के लिए यह रसीला व्यापार जब केवल एक गँवई वाली तक सीमित रह गया और उधर से प्रत्याशित प्रतिदान न मिलने से निराशा होने लगी, तब मेरी आँखें संस्कृत के समास से भोजपुरी के व्यास की ओर एकदम खिंच आईं। साहित्य का अधकचरा अध्ययन, मित्रों का प्रोत्साहन, पूरबी का स्नेहांचल विज़न और अपना बेकार जीवन...मेरे मध्य वित्तीय निबंधों को यही ध्यान मिला है। मैं पूर्वोक्त रससिद्ध लेखकों का ऋणी हूँ, यह कहकर उनको भी अपने साथ घसीटूँ, इतना दुस्साहस मुझमें नहीं है, किंतु जिन मित्रों ने मुझे इस ओर आने के लिए प्रोत्साहित क्यों दुरुत्साहित किया है, उनके नाम मैंने अपने आभार में गिना दिए हैं। व्यक्तियों के प्रभाव की बात तो यह हुई, जिन विचारों की छाप मेरे ऊपर मेरी जानकारी में पड़ी है, उनका भी कुछ ब्यौरा दे दूँ। व्यक्तिप्रधान निबंधों में कुछ लोग विचारत्व की ख़ास उपयोगिता नहीं देखते और वैसे लोगों को शायद मेरे निबंधों में विचारत्व दिखे भी न, परंतु मैं अपनी आस्थाओं का अभिनिवेश रखे बिना कहीं भी नहीं रहना चाहता, निबंध में तो और भी नहीं। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है, मैं रेती में अपनी डेंगी नहीं चलाना चाहता और न ज़मीन के ऊपर बने रुँधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। इसलिए प्रचलित शब्दावली में अगर प्रगतिशील नहीं हूँ, तो कम-से-कम प्रतिगामी भी नहीं ही हूँ। वैसे अगर भारत के राम और कृष्ण तथा सीता और राधा को प्रगति के दायरे से मतरूक़ न घोषित किया जाए, तो मैं भी अच्छा ख़ासा प्रगतिशील अपने को कह सकता हूँ, और अगर राम और कृष्ण के नाम के साथ प्रतिगामिता लगी हुई हो, तो मुझे प्रतिगामी कहलाने में सुख ही है। कुछ दिनों तक सम्मेलन की राजनैतिक गोलबन्दी में ज़रूर पड़ गया था, पर किसी साहित्यिक गोलबन्दी में मैं शरीक नहीं रहा हूँ। इसलिए न मुझको किसी का वरद हस्त प्राप्त है, न किसी के पूर्वग्रह का कड़वा घूँट ही। मानवता की समानभूमि पर मुझे सभी मिल जाते हैं। यों तो 'सहस नयन' 'सहस दस काना' और 'दो सहस' रसना वाले प्रणम्य महानुभाव जो न देख-सुन-कह सकें, उनसे मैं पनाह माँगता हूँ। इतना मैं और कह दूँ कि विलायती चीजों के आदान से मुझे विरोध नहीं है, बशर्ते उतनी मात्रा में प्रदान करने की अपने में क्षमता भी हो। इस सिलसिले में मुझे काशी के एक व्युत्पन्न पंडित के बारे में सुनी कहानी याद आ रही है। उन पंडित के पास जर्मनी से कुछ विद्वान आये (शायद उन दिनों जो विद्वान संस्कृत सीखने आते थे, उनका घर जर्मनी ही मान लिया जाता था, खैर) और उनके पास टिक गए। स्वागत-सत्कार करते-करते पंडित जी को एक दिन सूझ आई कि इन लोगों को भारतीय भोजन भारतीय ढंग से कराया जाए। सो वह इन्हें गंगा जी में नौका-विहार के लिए ले गए और गरमा-गरम कचालू बनवाकर भी लेते गए। नाव पर कचालू दोने में परोसा गया, पंडित जी ने भर मुँह-कौर कचालू झोंक लिया, इसलिए उनकी देखादेखी जर्मन साहबों ने भी काफ़ी कचालू एक साथ मुँह में डाला, और बस मुँह में जाने की देरी थी, लाल मिर्च का उनके संवेदनशील सुकंठ से संस्पर्श होते ही, वे नाच उठे और कोट-पैंट डाले ही एकदम गंगा जी में कूद पड़े। किसी तरह मल्लाहों ने उन्हें बचाया। पर इसके बाद उनका ‘अदर्शनं लोपः’ हो गया। दूसरे लोगों ने पंडित जी को ऐसी अभद्रता के लिए भलाबुरा कहा, तो उधर से जवाब मिला..."इन लोगों ने हमें अंडा-शराब जैसी महँगी और निशिद्ध चीजे़ं खानी सिखलाईं, तो ठीक और मैंने शुद्ध चटपटे भारतीय भोजन की दीक्षा एक दिन इन लोगों को देने की कोशिश की तो मैं अभद्र हो गया?", लोग इस उत्तर से निरुत्तर हो गए। तो कहने का मतलब यह कि आदान-प्रदान का यह भी एक तरीका है और शास्त्रसम्मत तरीका है, काशीधाम की इस पर मुहर लगी हुई है। परंतु मैं साहित्य में ऐसे आदान-प्रदान का पक्षपाती नहीं हूँ। सूफ़ियों और वेदांतियों के जैसे आदान-प्रदान का मैं स्वागत करने को तैयार हूँ, नहीं तो अपनी बपौती बची रहे, यही बहुत है। इस प्रसंग में आज नाम आता है, मार्क्स और फ्रायड का। अर्थ और काम के विवेचन में इनकी देन महनीय है, इसमें संदेह नहीं किंतु जब भारत में इनके अनुकूलन (एडाप्टेशन) की बात आती है, तो बरबस हमारा ध्यान अपने धर्म की ओर चला जाता है। 'रिलीजन' से 'धर्म' में कितना भेद है, यह जो नहीं जानता वह भारतीय संस्कृति की समन्विति का ठीक-ठीक साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। जन संस्कृति की बात भी जो लोग आज बहुत करते हैं, वे 'जन' का इतिहास परखे बिना ही। भारत का धर्म किसी शासन-व्यवस्था का कवच या आवरण नहीं है, वह स्वयं भारतीय जीवन का अंतर्मर्म है। उस धर्म के जितने लक्षण कहे गए हैं, सबमें से यही ध्वनि निकलती है "चोदना लक्षणो धर्मः", आगे बढ़ने की प्रेरणा धर्म है, "यतोऽभ्युदयनिः श्रेयः संसिद्धि स धर्मः" जिससे अभ्युदय और परम और विश्वव्यापी कल्याण हो, वह धर्म है। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों में समरसता स्थापित करने वाला माध्यम है। उस धर्म पर ऐंठन ज़रूर पड़ता गई, पर इन खोलों को चीरने के बजाय भारतीय जीवन के मूल को उखाड़ फेंकना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मार्क्स और फ्रायड की स्थापनाओं के शीर्ष पर व्यास का यह वाक्य मुझे झिलमिलाता मिलता है -
ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चित श्रृणोति माम्। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते।।
अर्थ और काम की आधार-रेखा के लिए धर्म ही शीर्षबिंदु है और सुघटित समाज के लिए तीनों का समत्रिकोण अत्यावश्यक है।
श्री मिश्र ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य के साथ-साथ भाषा विज्ञान के भी प्रकांड पंडित होने के नाते उन्हें भाषा और साहित्य जगत में हमेशा अग्रणी पंक्ति में ही रखा जाता है। उन्होंने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने, उसे समृद्ध करने और नवाचार तथा नए प्रयोगों से उसे और अधिक रोचक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने निबंधों और अन्य कृतियों में प्राचीन संस्कृत साहित्य को समसामयिक दृष्टि से देखते और उसमें से भी मानवता के मोती निकाल कर पाठकों को परोसते नज़र आते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव उनके निबंधों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रो० मिश्र जी का लेखन आधुनिकता की मार, देशकाल की विसंगतियों और मानव की यांत्रिक छटपटाहट का चरम आख्यान है, जिसमें वे पुरातन से अद्यतन और अद्यतन से पुरातन की बौद्धिक यात्रा करते नज़र आते हैं। "मिश्र जी के निबंधों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोकतत्व, बौद्धिकता, सर्जनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रम्यरचनात्मकता, भाषा की उर्वर सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता इन निबंधों में एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। मिश्र जी के निबंधों में बहुधा लोकजीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठता है। विशेष रूप से भोजपुरी लोकजीवन उनके निबंध में इस प्रकार समाया हुआ है कि उन्हें भोजपुरी का प्रतिनिधि निबंधकार कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।उनके निबंधों में रोजमर्रा के व्यावहारिक सरोकारों को भी इतनी चतुराई के साथ उकेरा गया है कि कुछ समालोचक तो उनकी तुलना अंग्रेज़ी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार फ्रांसिस बेकन से करने में भी संकोच नहीं करते हैं और कहते हैं कि पं० विद्यानिवास मिश्र के निबंध भी व्यावहारिक ज्ञान का अनोखा पुलंदा हैं।
श्री मिश्र ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य के साथ-साथ भाषा विज्ञान के भी प्रकांड पंडित होने के नाते उन्हें भाषा और साहित्य जगत में हमेशा अग्रणी पंक्ति में ही रखा जाता है। उन्होंने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने, उसे समृद्ध करने और नवाचार तथा नए प्रयोगों से उसे और अधिक रोचक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने निबंधों और अन्य कृतियों में प्राचीन संस्कृत साहित्य को समसामयिक दृष्टि से देखते और उसमें से भी मानवता के मोती निकाल कर पाठकों को परोसते नज़र आते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का प्रभाव उनके निबंधों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रो० मिश्र जी का लेखन आधुनिकता की मार, देशकाल की विसंगतियों और मानव की यांत्रिक छटपटाहट का चरम आख्यान है, जिसमें वे पुरातन से अद्यतन और अद्यतन से पुरातन की बौद्धिक यात्रा करते नज़र आते हैं। "मिश्र जी के निबंधों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोकतत्व, बौद्धिकता, सर्जनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रम्यरचनात्मकता, भाषा की उर्वर सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता इन निबंधों में एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। मिश्र जी के निबंधों में बहुधा लोकजीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठता है। विशेष रूप से भोजपुरी लोकजीवन उनके निबंध में इस प्रकार समाया हुआ है कि उन्हें भोजपुरी का प्रतिनिधि निबंधकार कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।उनके निबंधों में रोजमर्रा के व्यावहारिक सरोकारों को भी इतनी चतुराई के साथ उकेरा गया है कि कुछ समालोचक तो उनकी तुलना अंग्रेज़ी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार फ्रांसिस बेकन से करने में भी संकोच नहीं करते हैं और कहते हैं कि पं० विद्यानिवास मिश्र के निबंध भी व्यावहारिक ज्ञान का अनोखा पुलंदा हैं।
संदर्भ
- "चितवन की छांह" निबंध संग्रह की भूमिका से साभार।
लेखक परिचय
शिव कुमार निगमद्वितीय सचिव (हिंदी, शिक्षा एवं संस्कृति)
भारतीय उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन,
त्रिनिदाद और टोबैगो।
भारतीय उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन,
त्रिनिदाद और टोबैगो।




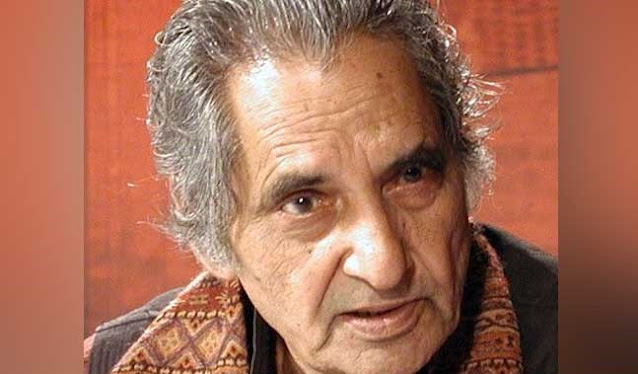
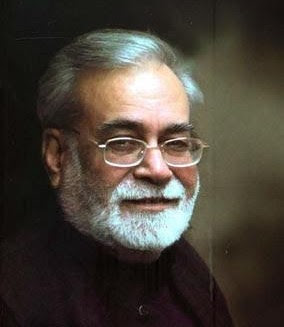












वाह...बहुत ही अच्छा .
ReplyDeleteअद्भुत आलेख, आदरणीय!
ReplyDeleteपं विद्यानिवास मिश्र हिन्दी के उन महान साहित्यकारों में परिगणित थे जिन्होंने अपने अमर कृतित्व से साहित्य-निधि को समृद्ध किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डा. मिश्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध लेखन की परम्परा को शिखरस्थ किया।
ReplyDeleteश्री शिव कुमार निगम ने ऐसी महान विश्व विभूति
के विराट व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व के विवेचित कर प्रबुद्ध पाठकों और अनुसंधित्सुओं के लिए चिन्तन और शोध का पथ प्रशस्त किया है।उनकी अमूल्य कृतियां सदैव चिन्तन को एक नया आयाम देती रहेंगी। हार्दिक बधाई!
डॉ.राहुल, नयी दिल्ली (भारत)
ReplyDeleteशिव कुमार निगम जी ने इस विस्तृत लेख के माध्यम से पं० विद्यानिवास मिश्र जी के जीवन एवं साहित्य पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। निगम जी को इस लेख के लिए हार्दिक बधाई।
ReplyDeleteहिंदी निबंध साहित्य के प्रतिष्ठित निबंधकार आदरणीय प. विद्यानिवास मिश्र जी ने सर्वाधिक संख्या में अपना निबंध संसार रचा है। उनके निबंध में भावात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक तथा हास्यव्यंगात्मक शैली की पात्रता होती थी। आप निबंध में छोटी गद्य रचना के अलंकारिक साहित्यकार थे। आदरणीय शिव कुमार निगम जी ने उनके साहित्यिक शैलीगत विशेषता को भली भांति दर्शाया है। आपके आलेख से प. मिश्र जी के भाषा और दृष्टिकोण के मौलिकता के दर्शन होते है। आपका लेख श्री मिश्र जी के निबंध के भावों के अनुरूप है जैसे वह अपनी शैली में प्रयोग किया करते थे। सुसंक्षिप्त और सुगठित आलेख के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हार्दिक शुभकामनाएं।
ReplyDeleteशिव कुमार जी, मैंने आपके लेख से कई बातों के बारे में पहली बार जाना, जैसे ललित निबंध, और पं. विद्यानिवास मिश्र जी की साहित्यिक विशेषताओं की विस्तृत जानकारी मिली। उत्सुकतावश ललित निबंध के बारे में विभिन्न स्रोतों से पढ़ा। इस लेख ने निश्चित ही मेरी जानकारी को समृद्ध किया है। आपको इसके लिए हृदयतल से आभार और बधाई।
ReplyDeleteइतने अच्छे आलेख के लिए शिवकुमार जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ।
ReplyDeleteइतने अच्छे आलेख के लिए शिवकुमार जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ।-सुनील
ReplyDelete