गुवाहाटी आने के बाद यदि ये चाहते तो एक प्रतिभाशाली मेधावी युवा होने के कारण कहीं अच्छी नौकरी पा सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा न करके, १९५५ में ‘द असम ट्रिब्यून’ अख़बार के उप-संपादक के रूप में काम प्रारंभ करके स्वयं को असमिया भाषा, पत्रकारिता और साहित्य को समर्पित करने का निर्णय लिया। आठ वर्ष बाद ‘द असम ट्रिब्यून’ छोड़कर अगले तीन-चार वर्ष एक अन्य अख़बार ‘असम बातोरी’ के संस्थापक-संपादक रहे। मासिक साहित्यिक पत्रिका ‘मणिद्वीप’ और ‘असमिया’ की भी दो-दो, तीन-तीन वर्ष पूरी क्षमता से सेवा की। क़रीब दस वर्ष, १९७६ से १९८५ तक, एक लोकप्रिय मासिक पत्रिका ‘प्रकाश’ के संस्थापक और संपादक के रूप में कार्य किया। साथ ही पाँच-छह वर्ष दैनिक 'नूतन’ का संपादन किया।
चन्द्रप्रसाद ने ख़ूब साहित्य पढ़ा। वे ‘महाभारत’ और ‘रामायण’ - इन दो प्राचीन महाकाव्यों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इन्हें केवल धार्मिक ग्रंथ न मानकर उनका आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंभीर विश्लेषण किया तथा उन पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखीं, जो ‘गरीयसी’ पत्रिका में शृंखलाबद्ध रूप से छपती थीं तथा बाद में अलग से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुईं। महाभारत के बारे में वे कहते थे, "यह महाकाव्य हमारे भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा करता रहेगा।"
भारतीय साहित्य में कर्ण पर लेखन की परंपरा सी बनी हुई है। अब तक कर्ण पर लिखी कई रचनाओं में से कुछ प्रमुख हैं - रबींद्रनाथ टैगोर की कविता ‘कर्ण-कुंती संवाद’, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ‘रश्मिरथी’, शिवाजी सावंत की पुस्तक ‘मृत्युंजय’ और मराठी लेखक रणजीत देसाई की कृति ‘राधेय’। इसी परंपरा में चन्द्रप्रसाद ने कर्ण के दुखद जीवन को आधार बनाकर ‘महारथी’ उपन्यास लिखा, जो साहित्य जगत में उनका अनूठा योगदान है। असमिया भाषा में कर्ण पर यह पहली रचना है। सैकिया ने पाठकों के लिए पहले से ज्ञात महाभारत की कहानी को मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि दी है। यह उपन्यास कर्ण के मुँह से कर्ण के जीवन की और कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत की कहानी है, जिनके साथ कर्ण के संबंध हैं, उनका विस्तृत विश्लेषण किया है। चन्द्रप्रसाद ने एकलव्य और कर्ण के औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों के शैक्षिक-परिदृश्यों के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं।
सैकिया ने इस उपन्यास में मानवता के पक्ष पर जोर दिया है। इसका एक उदाहरण है - आचार्य द्रोण द्वारा एकलव्य से उसका वंश पूछे जाने के जवाब में एकलव्य कहता है, “मैं एक मानव-बच्चा हूँ, यही मेरा वंश है। क्या मेरी इस पहचान से मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ?” चन्द्रप्रसाद ने कर्ण को प्रतीक बनाकर मनुष्य की सार्वभौमिक पहचान और अकेलेपन की व्यथा भी दिखाई है।
चन्द्रप्रसाद ने असम की बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वतंत्रता-सेनानी, लेखक, संगीतकार, चित्रकार, फ़िल्म-निर्माता, असम के सांस्कृतिक प्रतीक ज्योतिप्रसाद अगरवाला (अग्रवाल) से प्रभावित होकर उन पर एक जीवनीपरक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है - ‘तोरे मोर आलोकरे यात्रा (तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी की यात्रा)’। जैसे रबींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीतों को ‘रबींद्र-संगीत’ कहा जाता है, वैसे ही ज्योतिप्रसाद द्वारा रचित गीतों को ‘ज्योति-संगीत’ कहा जाता है। किताब का नाम ‘तोरे मोर आलोकरे यात्रा’ ज्योतिप्रसाद के एक गाने की एक पंक्ति पर रखा गया है। ‘तोरे मोर आलोकरे यात्रा’ पुस्तक के लिए चन्द्रप्रसाद को २००० के ‘प्रकाशन परिषद पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।
सैकिया के कार्यों से स्पष्ट दिखाई देता है कि जितना काम उन्होंने कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किया है, उससे कई गुणा अधिक अख़बारों और पत्रिकाओं के लिए किया है। साहित्यिक पत्रिका के क्षेत्र में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है।
नई लेखनी को प्रोत्साहन और प्रेरणा देना एक तरह से चन्द्रप्रसाद के जीवन का लक्ष्य बन गया था। उनके अख़बार और पत्रिकाएँ बहुत सारे नए पत्रकारों और साहित्यकारों के लिए प्रगति का प्रथम सोपान बने। कुछ लोग लेखन के क्षेत्र में बड़ी सहजता और सरलता से प्रवेश करके अपनी जगह आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लेखन-प्रतिभा होने के बावजूद झिझक उनके रास्ते का रोड़ा बन जाती है। चन्द्रप्रसाद बहुत सहज भाव से ऐसे लोगों को समझाते, उनसे कहते - ‘आप लिखिए, आगे मैं देख लूँगा।’ इनकी पत्रकारिता से प्रभावित एक बड़ा नाम है - प्रतिष्ठित असमिया लेखक होमेन बरगोहाईं। होमेन को अपने एक आलोचनात्मक लेख के चलते सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने चन्द्रप्रसाद से प्रभावित होकर उन्हीं के द्वारा संपादित एक अख़बार में काम शुरू किया। आगे उनका मन लेखन में ऐसा रमा कि उन्होंने विपुल साहित्य रचा और चन्द्रप्रसाद से भी पहले, वर्ष १९७८ में ‘पिता-पुत्र’ उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार होमेन बरगोहाईं ने ख़ुद यह बात कही थी कि उनके जीवन में एक दौर ऐसा था, जब उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएँ संपादक चन्द्रप्रसाद से प्रेरित होकर लिखी थीं।
सन १९६५-६६ में वे अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ६ महीनों के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ से हर सप्ताह लिखी उनकी चिट्ठी अख़बार में छपती थी। बाद में उन चिट्ठियों की ‘अमेरिका से चिट्ठी’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी।
चन्द्रप्रसाद सैकिया ने लगभग बीस वर्ष ‘असम प्रकाशन बोर्ड’ के सचिव-पद को सुशोभित किया। उनका वह कार्यकाल असम साहित्य के लिए सुनहरा काल साबित हुआ। सैकिया ने अपने कुशल नेतृत्व से असम प्रकाशन बोर्ड को असमिया साहित्य का तीर्थ बना दिया था। यदि वे असम प्रकाशन बोर्ड के सचिव न होते तो कौन जाने सत्रीय नृत्य, प्राच्य शासनावली, कौटिल्य-अर्थशास्त्र, ज्योतिप्रसाद रचनावली, कालीराम मेधी रचनावली, गुहाय्बरुआ रचनावली, हस्तिविद्यानवो और अन्य कई दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ असमिया पाठकों को उपलब्ध होते भी या नहीं।
‘असम प्रकाशन बोर्ड’ के सचिव के रूप में चन्द्रप्रसाद १९८३ में फ़्रैंकफर्ट विश्व-पुस्तक मेले के दौरे पर गए थे। उसके अगले वर्ष भारत के ‘नेशनल बुक ट्रस्ट’ के सहयोग से प्रथम गुवाहाटी पुस्तक मेले का आयोजन किया। इस प्रकार के आयोजनों से लोगों को किताबें पढ़ने और ख़रीदने के अवसर प्राप्त होते रहे और उनकी साहित्य में रुचि बढ़ती रही।
चन्द्रप्रसाद ने वर्ष १९९३ में असमिया भाषा में समाजोन्मुख साहित्यिक पत्रिका ‘गरीयसी’ की स्थापना की थी और वे जीवनपर्यंत उसके प्रमुख संपादक रहे। जल्दी ही यह पत्रिका असम की प्रमुख साहित्यिक पत्रिका बन गई। वे उसमें उभरते हुए साहित्यकारों की कृतियाँ छापते थे और उनके विकास की राह प्रशस्त करते थे। गरियसी ने बहुत नाम कमाया; इसे लगातार तीन वर्ष (१९९६-१९९८) ‘कथा’ पुरस्कार से नवाज़ा जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी इसकी गिनती असम की एक प्रमुख साहित्यिक पत्रिका के रूप में होती है।
असम साहित्य में पत्रिकाओं के नाम पर साहित्यिक-युग का नाम रखा गया है। जब चन्द्रप्रसाद सैकिया (१९९९ से २००१) ‘असम साहित्य सभा’ के अध्यक्ष थे, तब १९-वीं सदी में कोलकता से प्रकाशित दो पुरानी पत्रिकाओं ‘जोनाकी (चाँदनी)’ और ‘बांही(बाँसुरी)’ के अंकों के संकलन के प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण काम हुआ था।
क़रीब पिछले तीस वर्षों से असम में रह रहे और कार्यरत हिंदी कवि, अनुवादक, दैनिक अख़बार ‘सेंटीनल’ के पूर्व संपादक तथा वर्तमान में ‘दैनिक अरुण भूमि’ के सलाहकार संपादक श्री दिनकर कुमार चन्द्रप्रसाद सैकिया को व्यक्तिगत-रूप से जानते थे। उन्होंने उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी तस्वीर पेश की है - चन्द्रप्रसाद सैकिया हमेशा धोती-कुरता पहनने और मोटा चश्मा लगाने वाले समय के पाबंद, बहुत ही अनुशासित, प्रसन्नचित्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे।
चंदप्रसाद सैकिया मूलतः आशावादी थे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी निराश होना उनके स्वभाव में नहीं था। अपने इस गुण के लिए वे हमेशा याद किए जाएँगे। चन्द्रप्रसाद के समकालीन असमिया लेखक और उनके मित्र महिम बरा ने उनके बारे में कहा था - सैकिया में ‘आशावाद’ के संक्रामक वायरस हमेशा प्रचुर मात्रा में रहते थे।
जीवन के अंत तक वे अपनी आत्मकथा ‘आपोन सत्तार संधानत’ लिख रहे थे। वह गरियसी पत्रिका में शृंखलाबद्ध रूप में छप रही थी, लेकिन चन्द्रप्रसाद के वहाँ चले जाने से, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता, वह अधूरी रह गई, परिणामस्वरूप असमिया साहित्य एक बहुमूल्य कृति से वंचित रह गया।
चंदप्रसाद सैकिया ने असमिया साहित्य को आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध किया है। क़रीब पाँच दशकों तक असम के साहित्य संसार में उनके विपुल लेखन का वर्चस्व क़ायम रहा। असम में पत्रकारिता की पैठ मज़बूत करने में उनका योगदान अतुलनीय है; उन्हीं को सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादन का श्रेय जाता है। उन्हें असमिया पत्र-पत्रिकाओं का सर्वाधिक सफल संपादक माना जाता है। समाज में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सन २००७ में ‘पद्म भूषण’ की उपाधि से सुशोभित किया था।
सन्दर्भ
१. हिंदी कवि, अनुवादक, असम में दैनिक अख़बार ‘सेंटीनल’ के पूर्व सम्पादक तथा वर्तमान में ‘दैनिक अरुण भूमि’ के सलाहकार सम्पादक श्री दिनकर कुमार के साथ फ़ोन वार्ता।
२.https://www.indiaonline.in/about/personalities/writersandpoets/chandra-prasad-saikia
३. http://www.indianstudies.net/V2/n2/v2n210.pdf
४. https://thereaderwiki.com/en/Chandra_Prasad_Saikia
डॉ. सरोज शर्मा : भाषा विज्ञान (रूसी भाषा) में एमए, पीएचडी; रूसी भाषा पढ़ाने और रूसी से हिंदी में अनुवाद का अनुभव; वर्तमान में हिंदी-रूसी मुहावरा कोश और हिंदी मुहावरा कोश पर कार्यरत पाँच सदस्यों की एक टीम का हिस्सा।



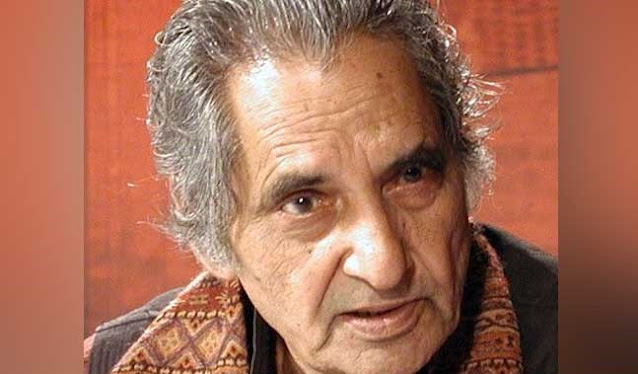
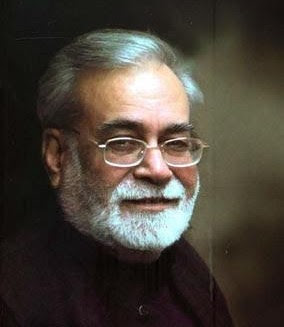











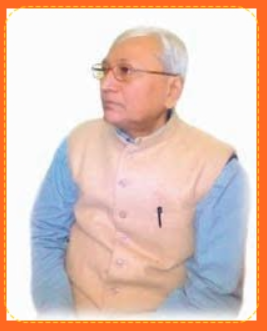

सरोज, सच कहा तुमने कि हम अपने देश की ही कितनी साहित्यिक विभूतियों से अपरिचित रह जाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विविधता हमारा गौरव है और उसकी पहुँच अधिकांश जनता तक हो तो सोने पे सुहागा हो जाए। चंद्रप्रसाद सैकिया जी को तुम्हारे आलेख के माध्यम से जाना, उनको और उनके अनुपम कृतित्व को जानना बहुत प्रेरणास्पद रहा। इस आलेख के लिए बहुत-बहुत बधाई और आभार।
ReplyDeleteनमस्कार सरोज जी
ReplyDeleteचंद्रा प्रसाद सैकिया जी के बहु आयामी व्यक्तित्व को आलोकित करते आलेख के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन। जितने बहु प्रतिभा के धनी सैकिया जी उतना ही विस्तृत और अद्भुत उनका साहित्यिक जीवन। लेखन, पत्रकारिता, प्रकाशक, संपादन के साथ संगीत और चित्रकारी में भी अनुभव रखने वाले सैकिया के बारे में आपकी कलम ने जो परिचय करवाया, उसके लिए आपका आभार। सदृढ़ और समृद्ध आलेख लेखन के लिए बधाई।
सारगर्भित और संग्रहणीय लेख।अभिनंदन।
ReplyDeleteप्रतिभा को सराहना प्रतिभावान का लक्षण होता है । सुंदर प्रस्तुति । मैं उड़िया हूँ, अहमिया भाषा मुझे आती तो आपको पढ़ने के बाद मैं महारथी के हिंदी रूपांतर में लग जाता । भारत के एक और सुयोग्य संतान से परिचित कराने के लिए धन्यवाद।
ReplyDeleteसंतोष मिश्
संतोष मिश्रा।
Deleteडॉ. सरोज जी नमस्ते। आपका लिखा चन्दप्रसाद सैकिया जी पर लेख पढ़ा। बहुत अच्छा लेख है। मेरे लिए तो नई जानकारी से परिपूर्ण लेख था। आपको इस रोचक एवं शोधपूर्ण लेख के लिए हार्दिक बधाई।
ReplyDeleteनमस्कार सरोज जी। सैकिया जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर सारगर्भित व रोचक आलेख। इस विभूति से परिचित कराने के लिए आपका आभार।
ReplyDeleteGood And Informative!🌹
ReplyDelete