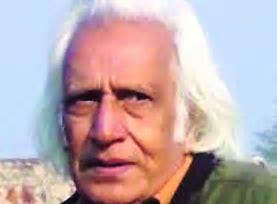
हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार श्री सुरेंद्र वर्मा का जन्म ७ सिंतबर १९४१ को उत्तरप्रदेश के झाँसी में हुआ। उनके चार भाई और एक बहन है। एक भाई रवींद्र वर्मा भी लेखक है। सुरेंद्र वर्मा ने शुरुआती दिनों में अध्यापन कार्य किया, बाद में कुछ कहानियाँ लिखीं। उन्होंने एक नाटककार के रूप में शुरुआत की थी। हिंदी नाट्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश की संवेदना को अग्रसर करने में इनकी भूमिका अहम रही है। उनका नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा के साथ लंबा संबंध रहा। फिल्म 'स्पंदन' के लिए स्क्रीन राइटिंग का नेशनल अवॉर्ड भी उन्हें मिला। दारा शिकोह पर बनाई गई उनकी डॉक्युमेंट्री पाँच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो चुकी है। उनका विवाह एक अमेरिकन स्त्री से हुआ, जो बाद में उनकी बच्ची को लेकर चली गई। असफल वैवाहिक जीवन के अकेलेपन से उत्पन्न पीड़ा की झलक इनके साहित्य में देखने को मिलती है।
साहित्यिक सफ़र
इनके नाटक नई सृजनात्मकता, सांकेतिकता, चित्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता, स्मृत्यावलोकन, मनोवैज्ञानिकता, वर्णनात्मकता के अद्भुत संगम हैं। पात्रों के संवादों में काव्यात्मकता सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की पहचान है। उनका प्रत्येक नाटक प्रयोग-धर्मिता का संकेत देता है। ऐतिहासिक और पौराणिक परिवेश के आधार पर उन्होंने जीवन की समस्त समस्याओं को उजागर किया है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आए परिवर्तन को भी उद्घाटित किया है और इनके माध्यम से अपने जीवन के अंतरंग अनुभवों को भी व्यक्त किया है। स्वतंत्रता पश्चात भारत के तेजी से बदलते मानवीय संबंधों के संघर्ष, स्त्री-पुरुष संबंधों की दरार, खालीपन, ऊब, परिवार-विघटन, दहेज-प्रथा, शोषित-नारी आदि इनके नाटक के पात्र हैं, जो समाज के दर्पण हैं। उनके नाटकों में कथानक की विशेषता है और अंत में कुछ नया देने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं।
विवाहोपरांत प्रेम-संबंधों को संपूर्ण सौंदर्य और गरिमा के साथ मंच पर साकार करने की अद्भुत क्षमता है। मूक गुड़िया की भाँति जीवन की अवहेलना करके अपनी समस्त सूक्ष्म भावनाओं को तिलांजलि देने वाली जैसी स्त्री उनके नाटकों की नायिका नहीं है। सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटकों में स्त्री को मनुष्य के रूप में देखते हुए स्त्री-आंदोलन को गति प्रदान की है। स्त्री को धरती, माता, देवी कहा गया; किंतु पुरुषों ने अपनी सुविधा-हेतु स्त्री को विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया, लेकिन अपने समान नहीं बनने दिया। सदियों से वह मात्र उपेक्षा और बंधनों को सहती दिखाई देती है। अब इन बंधनों और अत्याचारों का एहसास स्त्री को धीरे-धीरे होने लगा है और वह अपनी अस्मिता को पहचानने लगी है। उसकी लड़ाई अत्याचार के विरोध में जारी है। आज वह देवी नहीं, मनुष्य बनना चाहती है।
उनके पहले नाटक 'सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक' का अमोल पालेकर ने मराठी में मंचन किया, जिसका छः भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। सुरेंद्र वर्मा ने स्त्री-पुरुषों के संबंधों का निरूपण करते वक्त संयमित एवं काव्यात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है। संयम अभिव्यक्ति, अभिप्रेत के सटीक संप्रेषण की क्षमता और संवेदनशील काव्यात्मक भाषा के कारण उद्दाम-संभोग के प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रस्तुतीकरण के बावजूद यह नाटक कहीं से भी अश्लील या कुत्सित नहीं लगता। वे शीलवती के माध्यम से कहते हैं, "मर्यादा!… धर्म!… वैवाहिक संबंध।… सब मिथ्या।… सब पुस्तकीय…; लेकिन मुझे पुस्तक नहीं जीना अब।… मुझे जीवन जीना है।"
'शकुंतला की अंगूठी नाटक में स्पष्ट हुआ है कि व्यवसाय, कला से अधिक महत्त्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिक युग में कला पैसे के सामने बौनी है। नाटक में नाटककार ने रेखा की वाणी में काव्यात्मकता का प्रयोग किया है। 'एक दूनी एक' नाटक में आदमी के आंतरिक-पक्ष की कमजोरी तथा वेदना को प्रस्तुत करने के लिए काव्यों की रचना की है। इसमें अकेले रहने वाले स्त्री-पुरुषों की स्थिति वर्णित की गई है। उत्तर आधुनिकता ने सभी पुरानी मान्यताओं का खंडन कर दिया है। प्रेम केवल 'एडजस्टमेंट' है। इस नाटक में प्रेम के नाम पर दैहिक संबंधों को ही तरजीह दी गई है। 'कैद-ए-हयात' नाटक में नौशा मिर्जा गालिब के मुख से सचोट बात कह देने के लिए शायरी का प्रयोग किया है, जो नाटकीयता, काव्यात्मकता को सशक्तता से पेश करने में सक्षम है। 'छोटे सैयद बड़े सैयद' नाटक में काव्यात्मक भाषा में राजनीति, राजकीय कुचक्र, दाव-पेंच, हिंसा-घृणा, गठबंधन, रक्तपात, कुटिल चालों के वर्णन का चित्रण है।
'सेतुबंध' १९७२ ई० नाटक में नायक चंद्रगुप्त की महत्त्वाकांक्षाओं का बिंब है। नाटक में कालिदास और प्रभावती के गुरु-शिष्या संबंध होने के बावजूद प्रेम-संबंधों की बात की गई है। कालिदास का अपनी शिष्या के प्रति प्रेम-भाव भारतीय मूल्यों का विखंडन है। प्रभावती जब अपनी माँ से यह कहती है, "भावना के बिना शारीरिक संभोग बलात्कार होता है, और मैं उसी का परिणाम हूँ।"
प्रवरसेन की माँ बनकर भी वह पत्नी नहीं बन पाती। ऐसी स्थिति में यदि परपुरुष पति और पति परपुरुष बन जाए तो क्या आश्चर्य! आधुनिक जीवन का विवाह का 'काम' संबंधी समीकरण कुछ इस प्रकार है, "यदि पुरुष अविवाहित है तो स्त्री विवाहित, यदि पुरुष विवाहित है तो स्त्री अविवाहित।" 'सेतुबंध' नाटक की यही विडंबना है।
काम-चेतना के चित्रण के लिए सुरेंद्र वर्मा की जितनी तीखी आलोचना हुई, उतनी उन्हें अपार लोकप्रियता भी हासिल हुई। 'काम' वर्णन को हीन मानने वाली मानसिकता के विरोध में एक ऐसी रंगभाषा का निर्माण करते हैं, जो 'काम' की महनीयता को रंग-क्षेत्र में स्थापित करती है।
'द्रौपदी' नाटक आधुनिक जीवन की आपा-धापी, तनाव, संघर्ष, मन की टूटन, पारिवारिक विघटन, कुंठा आदि का वर्णन करता है। इसमें विवाहेतर जीवन की विसंगतियों से उत्पन्न त्रासदी है। सुरेखा के पति मनमोहन का व्यक्तित्त्व खंडित है। इसके कुत्सित रूपों का प्रतिबिंब उसके दोनों बच्चों (अलका, अनिल) के जीवन में पूर्णतः लक्षित होता है। साथ ही साथ भाई-बहिन, माता-पुत्री, पिता-पुत्री संबंधों का नया रूप भी है। 'आठवाँ सर्ग' नाटक का नायक कालिदास अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दवाबों से ग्रस्त है। नाटककार ने कालिदास के काव्य 'कुमारसंभव' के आठवें सर्ग में शिव और पार्वती की प्रेम-क्रीड़ाओं को साधारण पति-पत्नी के प्रेम-प्रसंगों के रूप में देखा और उसका वर्णन किया है, लेकिन धर्माध्यक्षों के द्वारा उसकी अश्लीलता पर आपत्ति की गई।
'अँधेरे से परे' एक समर्थ रचनाकार का अत्यंत सशक्त उपन्यास है, जो उनके सही अर्थों में सचेत कथाकार होने का एक मजबूत प्रमाण है। आज की मजबूर भागती-हाँफती ज़िंदगियों के आस-पास का बहुआयामी कथानक, उसकी तेज-टटकी, बेलौस भाषा और उसका शिल्पहीन शिल्प और कुल मिलाकर पूरे उपन्यास की बहुत भीतर तक बजती हुई गूँज 'अँधेरे से परे' के एक महत्त्वपूर्ण सार्थक उपन्यास होने-कहने के लिए काफी है। 'दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता' एक साँस रोककर पढ़ी जाने वाली कथा है, जिसमें सफेदपोश अपराधी और माफिया दोनों हैं। दो ज़िंदादिल मुंबई गए थे, मुर्दा बनकर रह गए। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा एक नई कथा-भूमि लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कृति ने न केवल पाठकों को मोहित किया वरन चौकायाँ भी। हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित 'व्यास सम्मान' ग्रहण करते समय सुरेंद्र वर्मा ने बताया, "मुगलकालीन नाटकों की शृंखला पर काम कर रहा था, लेकिन एक दिन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की इमारत में मुझे दुर्वासा ऋषि मिल गए और समझाने लगे कि साहित्य में उनके ऊपर काम नहीं हुआ है। मैंने कहा कि मैं तो मुगलों के वैभव को जी रहा हूँ। इस प्राचीन भारत पर क्यों काम करुँ? लेकिन इन ऋषि-मुनियों के पास बड़ी दैवीय ताकत होती है, जिसके चलते उन्होंने मुझसे कालिदास पर यह उपन्यास (काटना शमी का वृक्ष : पद्मपंखुरी की धार से) लिखवा ही लिया।" इस उपन्यास को लिखने में १० वर्ष का समय लगा।
प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का कहना है, "वर्मा क्लासिक लिखते हैं जो कम पठनीय होते हैं। उनका यह उपन्यास अपठनीय है, लेकिन इसमें शब्दों का उपयोग बहुत सोच-समझकर किया गया है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे रामचरित मानस में तुलसीदास ने शब्द-संयोजन किया है; और शायद यही वजह है कि उसे कई बार पढ़ा गया है। किसी कृति का सम्मान उसके बार-बार पढ़े जाने में है, और यह कृति वैसी ही है।"
हिंदी-नाट्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश की संवेदना को विकसित करने में सुरेंद्र वर्मा की प्रमुख भूमिका रही है।
सुरेंद्र वर्मा : जीवन परिचय |
जन्म | ७ सितंबर १९४१, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत |
शिक्षा |
स्नातकोत्तर | भाषा विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
साहित्यिक रचनाएँ |
उपन्यास | अँधेरे से परे (१९८०), नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली मुझे चाँद चाहिए (१९९३), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता (१९९८), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली काटना शामी का वृक्ष : पद्मपंखुरी की धार से (२०१०)
|
कहानी संग्रह | प्यार की बातें कितना सुंदर जोड़ा नई कहानियाँ
|
कविता संग्रह | |
व्यंग्य संग्रह | |
रूपांतर | |
विवेचन | |
नाटक | तीन नाटक (सेतबंधु, द्रौपदी, नायक खलनायक विदूषक) (१९७२) सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक (१९७५) आठवाँ सर्ग (१९७६) छोटे सैयद बड़े सैयद (१९८१) एक दूनी एक (१९८७) शकुंतला की अँगूठी (१९८७) क़ैद-ए-हयात (१९९३) रति का कंगन (२०११)
|
एकांकी संग्रह |
|
पुरस्कार व सम्मान |
केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, १९९३ साहित्य अकादमी पुरस्कार - 'मुझे चाँद चाहिए', १९९६ व्यास सम्मान, २०१६ फिल्म 'स्पंदन' के लिए स्क्रीन राइटिंग का नेशनल अवॉर्ड दारा शिकोह पर डॉक्युमेंट्री पाँच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल
|
संदर्भ
लेखक परिचय
संतोष भाऊवाला
आपकी कविताएँ-कहानियाँ कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, जिनमें से कई पुरस्कृत भी हैं। आप कविता, कहानी, ग़ज़ल, दोहा आदि लिखती हैं। रामकाव्य पियूष, कृष्णकाव्य पियूष व अन्य कई साँझा संकलन प्रकाशित हुए हैं।
ई-मेल - santosh.bhauwala@gmail.com
व्हाट्सएप - ९८८६५१४५२६




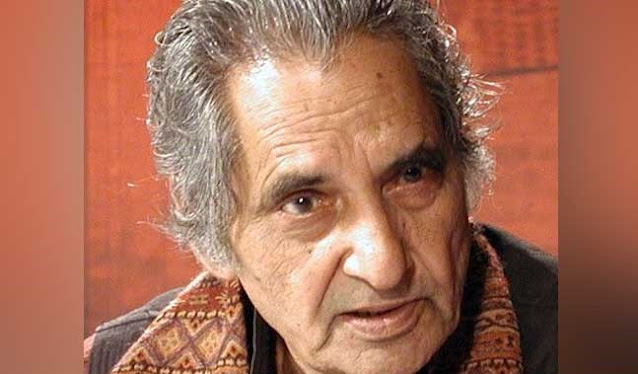
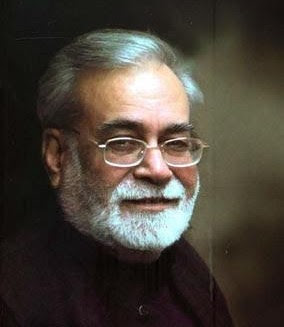











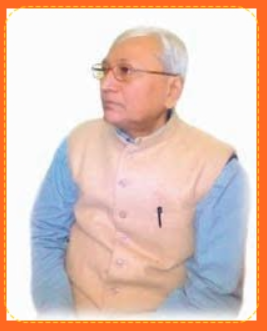

संतोष जी, आपने सुरेंद्र वर्मा जी के कृतित्व का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। उनका लेखन आसान नहीं, और उस पर लिखना तो बिलकुल आसान नहीं। आपको इस प्रस्तुति के लिए बधाई। 💐💐
ReplyDeleteमैंने बहुत वर्ष पहले “सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक “ पढ़ा था। बड़ा प्रभावशाली नाटक है। ऐसे विषम विषय पर ऐसी शास्त्रीय विवेचना कठिन काम है। हिंदी में कठिन काम करने वाले लेखक हमेशा हुए हैं। 😊💐
हरप्रीत जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आलेख का ताज है जिसके बिना आलेख अधूरा लगता है |
Deleteसंतोष जी नमस्ते। आपने सुरेंद्र वर्मा जी पर अच्छा लेख लिखा है। उनका साहित्य सृजन विस्तृत एवं बहुआयामी है जो पाठकों को खूब भाता है। आपने उनके साहित्य एवं जीवन के परिचय को लेख में बखूबी पिरोया। आपको इस बढ़िया लेख के लिए हार्दिक बधाई।
ReplyDeleteसंतोष जी, अभी आपका आलेख पढ़ा। जिस बेबाकी से सुरेंद्र वर्मा जी सामाजिक सच्चाई के बारे में लिखते थे, उसकी विसंगतियों की परतें अपनी रचनाओं में उधेड़ कर रख देते थे, अपने भी उसी शिद्दत से खूब खोज करके अपना यह आलेख लिखा है। आप द्वारा उद्धृत उदाहरण सुरेंद्र वर्मा जी के कृतित्व और कलम से अच्छा परिचय करते हैं। इस सुन्दर भेंट के लिए आपको साभार बधाई
ReplyDelete