
कुशारी से टैगोर तक का सफ़र
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के पूर्वज हजारों साल पहले वर्तमान
उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िला में बस गए थे। गंगा किनारे बसा यह ब्राह्मण परिवार अंग्रेज़
अफसरों को नदी पार करने के लिए नाव उपलब्ध कराता था। अपने कारोबार को बढ़ाने के
उद्देश्य से पंचानन कुशारी नामक एक दक्ष ब्राह्मण कलकत्ता आए और यहाँ ईस्ट
इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज़ व्यापारियों के साथ व्यापर करने लगे। वे कलकत्ता के
बंदरगाहों और कम्पनी को रोज़मर्रा की चीजें और नावें मुहैया कराते थे। व्यापार बढ़ने
लगा तो उन्होंने कलकत्ता के गरीब तबके के लोगों से काम लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों
से हर वक़्त दबे-कुचले औए सहमे-से रहने वाले इन मजदूरों के बीच पंचानन कुशारी ईश्वरीय
छवि वाले व्यक्ति बन गए जिन्होंने गरीबों को खुले हाथों से धन दिए और जिनका ‘गोरे
अफसरों’ के साथ रोज़ाना उठना-बैठना था। आदर और आस्था ने उन्हें ‘कुशारी’ से ‘ठाकुर’
बना दिया और धीरे-धीरे ‘ठाकुर’
उनकी पहचान का अटूट हिस्सा बन गया। अंगेज़ हुक्मरानों को ठाकुर का उच्चारण करने में
कठिनाई होती थी सो वे उन्हें टैगोर बुलाने लगे। इस तरह एक दक्ष ब्राह्मण परिवार
पहले ठाकुर और फिर टैगोर के नाम से विख्यात हुआ।
गुरुदेव का जन्म एवं बचपन
पंचानन ठाकुर की पाँचवीं पीढ़ी के रूप में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का
आगमन हुआ। उनकी पीढ़ी तक आते-आते यह ठाकुर परिवार कलकत्ता के रईस और प्रतिष्ठित
परिवारों में गिना जाता था और समूचे बंगाल में इनकी पहचान थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर
के पितामह द्वारिकानाथ ठाकुर ने अपने समय में ढ़ेरों संपत्ति अर्जित की थी। उनके
पास हजारों एकड़ ज़मीन,
चाय के बागान,
चीनी और नील की मिलें और सैकड़ों मालवाहक जहाज़ और नावें थीं। यह सारा कारोबार वे ‘टैगोर
एण्ड कम्पनी’ के नाम से करते थे। प्रिंस द्वारिकानाथ ने कोलकाता में अनेक बड़े
प्रतिष्ठानों जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज की नींव रखी थी। साथ
ही कई वैज्ञानिक संस्थानों यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक
सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
इनके पुत्र और रवीन्द्रनाथ के पिता देवेन्द्रनाथ एक सन्यासी प्रवृत्ति के मनुष्य
थे और समाज-सुधार के कार्यों में अधिक रूचि लेते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर और पिता
द्वारिकानाथ के गहरे दोस्त राम मोहन राय से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रह्म-समाज की
ओर रुख किया और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। कुछ
वर्ष सन्यासी जीवन जीने के बाद वे अपना राज-पाट सँभालने वापस तो आ गए किन्तु
व्यापर से अधिक उन्हें कला एवं संगीत में रूचि रहती। इसी बीच ७ मई १८६१ को जोरासांको
के महलनुमा घर में देवेन्द्रनाथ ठाकुर और पत्नी शारदा देवी की चौदहवीं संतान के
रूप में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। माँ की तबीयत ख़राब रहती थी, अतः उनका
लालन-पालन नौकरों द्वारा किया गया। उन्हें कभी वात्सल्य प्रेम का अनुभव ही नहीं हुआ।
नटखट रवीन्द्र की शैतानियों से तंग आकर उन्हें पालने वाले नौकर ने उन्हें रामायण
की सीता-हरण का प्रसंग सुनाकर लक्ष्मण-रेखा में कैद कर दिया। इस बात का उनके बालमन
पर बहुत गहरा असर पड़ा जिसका ज़िक्र आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया – “हम नौकर शासन में जिए। हमारे मन को बिलकुल
जकड़ दिया गया था। हमारे नौकर श्याम ने लक्ष्मण-रेखा से बाहर निकलने पर चेतावनी दी
थी – घेरे से बहार निकलते ही बड़ी मुसीबत होगी। मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता
रहा। हमारे पास कपड़े-लत्ते एक-दो जोड़ी ही थे। दस साल तक होने तक मैंने मोज़े नहीं
पहने। एक जोड़ी स्लीपर थे जो पैर से बहुत बड़े थे।”
परिवार की परम्परा के अनुसार रवीन्द्रनाथ की प्रारम्भिक
शिक्षा घर पर ही आरम्भ हुई। पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। एक बार स्कूल जाने की हठ
करने पर मास्टर जी ने बहुत पिटाई कर दी। इस बात का भी उन्हें गहरा सदमा लगा। फिर
उनका दाखिला ‘द ओरिएण्टल सेमिनरी स्कूल’ में कराया गया। वहाँ भी शिक्षक विद्यार्थियों
को छड़ी से मारा करते थे। विद्या के मंदिर में शिक्षकों का ऐसा व्यवहार बालक
रवीन्द्र की समझ से बाहर था। फिर उनका दाखिला एक अंग्रेज़ी स्कूल ‘द बंगाल अकेडमी’ में
हुआ जहाँ उनपर अंग्रेज़ी पढ़ने का दबाव था। उनका मन अब स्कूलों से ऊब चुका था और
उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता था। लोग मज़ाक में उन्हें ‘स्कूल पलानो छेले’ यानि ‘स्कूल से भागने
वाला लड़का’ बुलाने लगे थे। ऐसे में संत प्रवृत्ति वाले पिता ने उन्हें हिमालय की
यात्रा पर चलने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मात्र ११
वर्ष की आयु में हिमालय की उस कठिन यात्रा ने रवीन्द्रनाथ के जीवन की दिशा बदल दी।
इस यात्रा का पहला पड़ाव ‘शान्तिनिकेतन’ था जो आगे चलकर रवीन्द्रनाथ की कार्यस्थली बनी।
दूसरा पड़ाव ‘अमृतसर’
शहर था। यहाँ जितने भी दिन रहे,
हर रोज़ स्वर्ण-मंदिर में मत्था टेकने जाते और गुरबाणी सुनते। बाबा गुरुनानक के
वचनों का उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। अमृतसर से निकलकर वे सात हज़ार फ़ीट की
ऊँचाई पर बसे डलहौज़ी पहुँचे – बिलकुल हिमालय की गोद में। यात्रा के दौरान पिता ने
उन्हें संस्कृत, अंग्रेज़ी,
बांग्ला,
धर्म,
आध्यात्म और खगोल-विज्ञान की शिक्षा दी। संस्कृत में उपनिषद् और रामायण की एक-एक
लाइन उन्हें मुँह-ज़बानी याद हो गई। पिता के साथ बिताए उन चंद महीनों ने उनकी सोच
और संस्कारों पर अमिट छाप छोड़े। जब वे हिमालय से लौटकर आए तब उनके व्यक्तित्व को
एक नई आभा मिल चुकी थी। अब लोग उन्हें सम्मानित नज़रों से देखने लगे थे। महिलाएँ
उनसे हिमालय-यात्रा के किस्से सुनतीं और संस्कृत में रामायण पाठ सुन मंत्रमुग्ध
होती थीं। माँ शरदा भी पुत्र की इस विलक्षण प्रतिभा से अभिभूत थीं। इसी समय, मात्र बारह वर्ष की
आयु में उन्होंने अपनी पहली लम्बी कविता ‘अभिलाषा’ लिखी जो ‘तत्वबोधिनी’ पत्रिका में प्रकाशित
हुई। एक बार फिर उनके पिता ने उनका दाखिला ‘सेंट ज़ेवियर’ स्कूल में करा दिया किन्तु
१८७५ में रवीन्द्रनाथ ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसी बीच माँ शारदा बीमार पड़ गयीं और
८ मार्च १८७६ को संसार छोड़ गयीं। माँ के जाने का दुःख उन्हें जीवन भर सालता रहा
लेकिन माँ की कमी पूरा करने घर में कादम्बरी भाभी का आगमन हुआ। रवीन्द्रनाथ से
थोड़े ही बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर की ब्याहता के रूप में कादम्बरी का गृह आगमन
घर में ख़ुशी के पल लेकर आया। कादम्बरी रवीन्द्रनाथ की हमउम्र थीं और साहित्य-कला
में रूचि रखती थीं। उनके आने से रवीन्द्र की क्रियात्मकता और सृजनात्मकता को मानो
चार चाँद लग गए थे। भाई ज्योतिन्द्र भी कविताएँ लिखते थे सो भैया-भाभी के साथ उनकी
मंडली जम गई थी। वे घंटों अपनी कविताओं पर बातचीत करते और नई रचनाओं की ओर प्रेरित
होते रहे। चौदह वर्ष की आयु में रवीन्द्र ने सोलह सौ पंक्तियों की एक अन्य कविता ‘बनफूल’ लिखी। यह कविता ‘ज्ञानान्कुर’
नामक पत्रिका में छपी और इसे भी खूब सराहना मिली। एक अंग्रेज़ अफसर के दिल्ली दरबार
लगाने की घटना पर उन्होंने एक व्यंग्य रचना कर उसका पाठ किया जिसकी चर्चा दूर-दराज़
तक हुई और लोग खोज-खोजकर रवीन्द्र की कविताएँ पढ़ने लगे। सोलह वर्ष की आयु में
उन्होंने पहली लघु-कथा ‘भिखारिनी’
लिखी। १८७८ में उन्होंने ‘कवि कहानी’
नाम से एक लम्बी कविता लिखी। कविता-कहानियों में रवीन्द्र ऐसे खो गए थे कि उनके
करियर को लेकर उनके बड़े भाई चिंतित हो गए। एक बड़े भाई सत्येन्द्रनाथ गुजरात के
अहमदाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज थे और उन्होंने रवीन्द्र को अपने पास बुला लिया। यहाँ
रहते हुए रवीन्द्र का परिचय यूरोपीय और पश्चिली साहित्य से हुआ। चार महीनों में उन्होंने
ढ़ेरों अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ डाली किन्तु बोल-चाल में बांग्ला उच्चारण उन्हें सहजता
से अंग्रेज़ी नहीं बोलने देता था। बड़े भाई ने इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें
अपने एक मराठी मित्र आत्माराम पांडुरंग के पास बॉम्बे (अब मुम्बई) भेज दिया। यहाँ
पांडुरंग की बेटी अन्नपूर्णा,
जो इंग्लैण्ड से पढ़कर लौटी थी,
ने रवीन्द्रनाथ की अंग्रेज़ी की क्लासेज़ ली और उन्हें फर्राटेदार अंगेज़ी सिखाई। वे
अन्नपूर्णा से इतने प्रभावित हुए कि उसे एक नया नाम दिया – नलिनी – जो आगे चलकर
उनकी कहानियों में नायिका के रूप में आईं।
अब तक रवीन्द्र सत्रह वर्ष के हो चुके थे और जीवन के अधिकतम वर्ष उन्होंने यायावरी में ही गुज़ारे थे। इसी बीच जज सत्येन्द्रनाथ का तबादला ब्राइटन, इंग्लैण्ड में हो गया और वे रवीन्द्र को अपने साथ उनकी पहली विदेश यात्रा पर ले गए। यहाँ रवीन्द्र ने लन्दन युनिवेर्सिटी में प्रवेश लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ एक आयरिश परिवार के घर पेइंग गेस्ट रहते हुए उन्होंने विधिवत् आयरिश संगीत सीखना शुरू कर दिया। कलकत्ता में उनके परिवार को जब इस बात का पता चला तो घबराकर उन्होंने रवीन्द्र को वापस भारत बुला लिया। इस चक्कर में उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। उनकी नाटक ‘भग्न हृदय’ (टूटा दिल) जिसे उन्होंने लन्दन प्रवास के दौरान शुरू किया था, वह भी बाद में भारत आकर पूरी की। किन्तु, कहते हैं न, कोई भी ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। जिस संगीत के सिखने पर घरवालों ने ऐतराज़ किया था, आगे चलकर उसी आयरिश संगीत का प्रयोग उन्होंने अपने नृत्य-नाट्य 'वाल्मीकि प्रतिभा' में किया था जिसकी सराहना करते घरवाले नहीं थकते।
परिवार के बुलाने पर वे कलकत्ता वापस आ तो गए थे किन्तु यहाँ उन्हें अकेलेपन ने फिर से घेर लिया। परिवार के अधिकतम सदस्य कलकत्ते से बाहर रहते थे और मन बहलाने के लिए उनका कोई संगी-साथी भी नहीं था। इसी दौर में उन्होंने उदास गीतों का एक संसार रचा जो ‘संध्या-संगीत' के नाम से प्रकाशित हुआ। साथ ही दो संगीत-नाटक 'वाल्मीकि प्रतिभा' और 'काल मृगया' लिखे जिसे खूब लोकप्रियता मिली। यह दौर रवीन्द्रनाथ की लेखनी का स्वर्णिम दौर था जब उन्होंने अपने जीवन के कई यादगार और नायाब रचनाओं का सृजन किया। बालिग होने पर ९ दिसम्बर १८८३ को उनका विवाह ग्यारह वर्षीया ब्राह्मण कन्या ‘भवतारिणी’ के साथ कर दिया गया जिसे परिवार ने ‘मृणालिनी’ नाम दिया। मृणालिनी अनपढ़ थीं और उनकी उम्र भी बहुत कम थी जिससे रवीन्द्रनाथ खुश नहीं थे किन्तु आगे चलकर मृणालिनी ने स्वयं को इस परिवार के अनुसार ढाल लिया – पहले बांग्ला और फिर अंग्रेज़ी सीखकर वे रवीन्द्र के मन में अपने लिए प्रेम और आदर जगाने में कामयाब रहीं। इसी बीच १९ अप्रैल १८८४ को एक अप्रत्याशित घटना ने एक बार फिर रवीन्द्रनाथ को मायूसी और उदासी में डुबो दिया जब उनकी सबसे प्रिय भाभी कादम्बरी ने आत्महत्या कर ली। बच्ची पत्नी से मन का दर्द बाँट न सके लिहाज़ा स्वयं को सृजन के संसार में डुबोते चले गए। अभिनय करना, कहानियाँ लिखना, नाटक और गीत लिखना इस समय चरम पर था। साथ ही आध्यात्मिक व सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना उन्हें सुकून देता था। पिता ने ब्रह्म समाज का सचिव बना दिया था सो धीरे धीरे उनका दुःख कम होता गया और वे सृजनात्मक कार्यों में लीन होते गए। उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। वे शिक्षा में कट्टरता के खिलाफ थे और भारतीय तथा पश्चिमी शिक्षा पद्धति दोनों के दोषों पर खुलकर लिखते थे। इन व्यग्यों ने उन्हें देश-विदेश में पठनीय बना दिया था। इधर उनका परिवार बढ़ा और उधर उनकी लेखनी नई-नई रचनाओं का सृजन करती रही। एक से बढ़कर एक कहानियों और कविताओं से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। वे परिवार से प्रकाशित पत्रिका ‘भारती’ के संपादन का कार्य भी देखते थे और स्वयं ‘बालक’ नाम की एक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका की ख़ासियत थी बाल मनोविज्ञान का गहराई से विश्लेषण। १८९४ से १९०० के बीच लिखी कविताओं का संग्रह जब बाज़ार में आया तब रवीन्द्रनाथ के नाम की धूम मच गई। फिर क्या था – एक के बाद एक कहानियों का ताँता सा लग गया – पोस्टमास्टर, चित्रा, नदी, चैताली, बैकुण्ठकथा, चिरकुमार सुधा और काबुलीवाला। काबुलीवाला तो मानो घर-घर में पढ़ा गया, इसपर फ़िल्में बनीं। आज भी स्कूल की किताबों में काबुलीवाला की कहानी शुमार है। १८९८ के जनांदोलन में अपने क्रान्तिकारी भाषणों और देशभक्ति के लेखों (कंठरोध) से रवीन्द्रनाथ जनता के बीच आ गए। नई सदी का स्वागत उन्होंने एक लम्बी कविता ‘सदी का अंत’ लिखकर किया।
१९०० का आगमन रवीन्द्र के जीवन में नए सृजन का एक पूरा संसार लेकर आया। १९०१ में ही उनके दो उपन्यास नष्टनीड़ और चोखेरबाली प्रकाशित हुए जिनपर क्रमशः चारुलता और चोखेरबाली फ़िल्में बनीं जिसे बहुत लोकप्रियता भी मिली। भारतीय विद्यालयों से बेज़ार रवीन्द्रनाथ ने २२ दिसम्बर १९०२ को शान्तिनिकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की जो आज भी अपनी साख और गरिमा के साथ कार्यशील है। किन्तु इन सब के बीच, १९०२ में पत्नी मृणालिनी एक लम्बी बीमारी के बाद बीस वर्षों की गृहस्थी को छोड़कर शरीर त्याग कर गईं। पत्नी वियोग में रवीन्द्रनाथ ने सत्ताईस कविताओं की एक शृंखला लिखी जिसे नाम दिया – स्मरण। दुःख का सिलसिला अभी थमा न था – १९०३ में तेरह वर्षीया पुत्री रेणुका और १९०५ में पिता ने साथ छोड़ दिया। दो वर्ष बाद १९०७ में उनका छोटा बेटा शमीन्द्रनाथ तेरह साल की उम्र में ही हैजे से मर गया। एक-एक करके अपने प्रियजनों की मौत ने मानों उन्हें तोड़ दिया था। किन्तु वे रवीन्द्र थे - टूटना मानो उन्होंने सीखा ही न था। हर झटके का सामना करने के लिए वे कलम का सहारा लेते थे। इस बार भी यही कलम और बच्चे उनकी साहस बनकर उनके साथ खड़े रहे। इसी समय उन्होंने बच्चों के लिए एक नाटक ‘शरदोत्सव’ लिखा जिसकी लोकप्रियता आज तक बनी हुई है, जो आज भी उसी उल्लास के साथ मंचित किया जाता है।
व्यक्तिगत जीवन की उहापोह के बीच अंगेज़ी हुकूमत की तानाशाही उन्हें नागवार गुजरी और उनकी कलम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आग उगलने लगी।
नोट : आलेख का दूसरा भाग : https://hindisepyarhai.blogspot.com/2022/05/blog-post_13.html
सन्दर्भ
- गुरुदेव, दिनकर जोशी
- विरासत – रवीन्द्रनाथ टैगोर; राज्यसभा टीवी
- https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-33543786
- विकिपीडिया


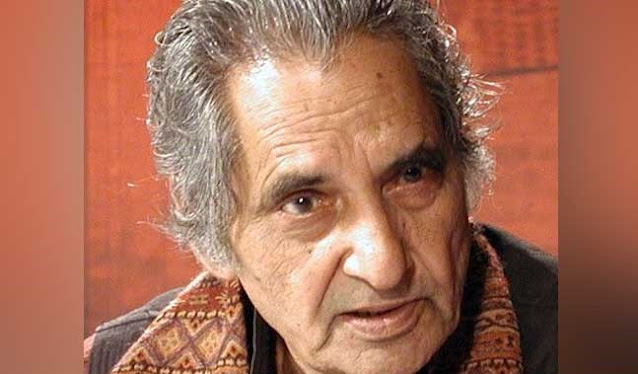
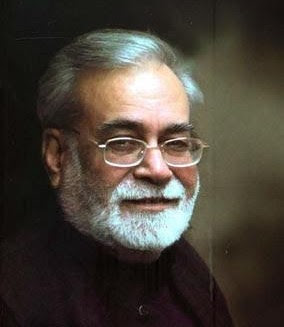













संग्रहणीय लेख।अभिनंदन।
ReplyDeleteकविवर रबींद्रनाथ ठाकुर की जीवन और साहित्यिक यात्रा का वर्णन करता अच्छा आलेख, इसके दूसरे भाग और इसके लेखक को जानने का इंतज़ार रहेगा। बेहतरीन लेखन के लिए बधाई और आभार।
ReplyDeleteगुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर पर बहुत जानकारी भरा लेख। इस महत्वपूर्ण लेख के लिये लेखक को बहुत बहुत बधाई।
ReplyDeleteगुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर बेहद रोचक आलेख। एक बार शुरू कर पाठक से छूट नहीं सकता। लेखक को किसी व्यक्ति की कहानी कहने का कमाल कौशल है। बधाई। दूसरे भाग की आतुर प्रतीक्षा। 💐💐💐
ReplyDeleteदीपा जी,
ReplyDeleteआपके द्वारा लिखित आदरणीय टैगोर जी पर दोनों लेख इतने जबरदस्त शब्दसंकल्पना और संयमता के साथ लिखा गया है कि सराहना के लिए शब्द कम पढ़ रहे है। अत्यंत खोजबीन के बाद लिखा गया यह लेख शब्दसिमित होते हुए भी निखर कर आ रहा है। *“सिर्फ किनारे पर खड़े रहकर समुंदर पार नहीं किया जा सकता"* टैगोर जी के इस कथन को साक्ष्य करता हुआ यह लेख रचा गया है कि अपनी रचनाओं को अमर बनाना है तो पढ़ना और टिका या प्रतिक्रिया देने से कुछ नही होगा उसके लिए कड़ी मेहनत, सुपरिचित, सुप्रचलित, सुभावार्थ, सुंदर शब्दश्रंखला और लेखन के प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है। आपकी लेखनी और ज्ञानवर्धक आलेख को सलाम। आभार आपका। अनगिनत शुभकामनाएं। प्रणाम।