टूटी साइकिल, सीट का उखड़ा कवर, पैडल नहीं, केवल उसका ढाँचा, साइकिल पर फटे पाँयचों वाली पतलून पहने, ‘न्यू एज’ की प्रतियाँ ग्राहकों तक पहुँचाने वाले तथा कच्चे मकान, अभावग्रस्त मोहल्ले, पानी के लिए चौराहे पर बने सार्वजनिक नलके की लाइन में लगने वाले जबलपुर के हाईस्कूल के टीचर। ये मुक्तिबोध थे, ‘तार सप्तक’ के पहले जाज्वल्यमान कवि। न केवल कवि, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार...बल्कि ऊबड़खाबड़ जीवन जीने वाले ऊबड़खाबड़ रचनाकार। उनकी कविताएँ रोंगटे खड़े कर देती हैं। जितना उन्होंने लिखा, उससे अधिक उनके बारे में दूसरे लेखकों द्वारा लिखा गया है।
गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी कविता ‘हर चीज़ जब अपनी’ में कहते हैं – ‘उनके साथ मेरी पटरी बैठती है, हाँ उन्हीं के साथ/ मेरी यह बिजली भरी ठठरी लेटती है’, ऐसे ही मुक्तिबोध के साथ हमारी पटरी बैठती है इसलिए जितनी बार उन्हें पढ़ा जाए, उतनी बार उनके लिखे के नए अर्थ खुलते हैं। वे कहते हैं ‘याद रखो कभी अकेले में मुक्ति न मिलती, यदि वह है तो सबके साथ ही है’। यह सर्वहारा का कवि है। मुक्तिबोध की कविताएँ किसी एक युग की कविताएँ भर नहीं हैं, बल्कि हर युग की भीतरी कसमसाहट और उद्वेलन की कविताएँ हैं। वर्गचेतना से भरी उनकी कविताएँ हर देश के बेबस की कविताएँ हैं। जैसे ये पंक्तियाँ- ‘लंदन का मज़दूर, फ्रांसीसी गुरिल्ला, युवजन, घूर-घूर वाशिंगटन देखता था’। उनकी कविता ‘भूल ग़लती’ में वे लिखते हैं, ‘भूल मेरी अपनी कमज़ोरियों के स्याह ज़िरहबख़्तर पहन’...और एक अन्य कविता में वे कहते हैं ‘इस सल्तनत में हर आदमी/ उचककर चढ़ जाना चाहता है/ धक्का देते हुए बढ़ जाना चाहता है/ हर एक को अपनी- अपनी पड़ी है/ चढ़ने की सीढ़ियाँ सिर पर चढ़ी हुई हैं’। उनकी कविताएँ हर व्यक्ति की कविता है इसलिए हर व्यक्ति उनकी कविताओं से जुड़कर पूछ बैठता है ‘पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है’? राजनीतिक सजगता उनकी विशेषता है।
मुक्तिबोध को पढ़ते हुए हर बार लगता है ‘अभिव्यक्ति के ख़तरे’ उठाने ही होंगे। उनकी कहानियाँ पाठक को भीतर तक हिलाकर रख देती हैं। ‘एक साहित्यिक की डायरी’ तथा ‘पक्षी और दीमक’ भ्रष्टाचार पर लिखी कहानियाँ हैं। ‘विपात्र’ नामक लंबी कहानी हो या ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ या ‘भूत का उपचार’- जैसी हर कहानी हमें अपने ही गिरेबान में झाँकने पर मजबूर करती है। ‘समझौता’ कहानी सर्कस कंपनी को ज़रिया बनाकर ‘कराह सुन कैसे चाबुक का ग़ुस्सा तेज़ हो जाता’ बता जाती है। मध्यमवर्गीय मानसिकता ‘जंक्शन’, ‘भूत का उपचार’ और ‘दाखिल दफ़्तर साँझ’ कहानियों में है। ‘प्रश्न’ कहानी में नैतिकता और अनैतिकता के बीच का संघर्ष है। जनसाधारण का विवशताग्रस्त जीवन ‘काठ का सपना’ में है। मुक्तिबोध के जीवन काल में भारत की आज़ादी, आज़ादी के बाद का स्वप्न-भंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीवादी ताकतों का मज़बूत होना और द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी कई ऐतिहासिक घटनाएँ हुईं, जो मुक्तिबोध की राजनीतिक टिप्पणियों में झलकती हैं। ‘क्लॉड ईथरली’ कहानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दस्तावेज़ है। आर्थिक विघटन का संत्रास ‘उपसंहार’ कहानी में है।
आत्म संघर्ष की तीव्रता में मुक्तिबोध कहते हैं ‘कवि भाषा का निर्माण करता है, जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निस्संदेह महान होता है’। उन पर दस्तायेव्स्की, फ्लैबेयर, गोर्की, इमर्सन का प्रभाव दिखता है। उनकी कविताओं में आत्मभर्त्सना, तनाव और द्वंद्व हैं। ‘तार सप्तक’ में अज्ञेय कहते हैं कि ‘मुक्तिबोध बात सीधी न कहकर सूचित करते हैं’। ‘तार सप्तकीय’ वक्तव्य में मुक्तिबोध लिखते हैं ‘मेरी ये कविताएँ अपने पथ ढूँढ़ने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं’। ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ में मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन सब नज़र आता है। डायरी के ‘तीसरा क्षण’ शीर्षक लेख में कला के तीन क्षण द्वारा फैंटसी की अवधारणा पर विचार है। ‘दूर तारा’ कविता में छायावाद नहीं, बल्कि शक्ति है। वे छायावाद के बाद की नई कविता के कवि हैं। उनकी ‘अंधेरे में’ नामक कविता बहुत लंबी है, उसमें जैसे आज़ादी के बाद के दो दशकों का इतिहास हो। अशोक वाजपेयी लिखते हैं ‘एक तरह से मुक्तिबोध की सारी कीर्ति, मरणोत्तर कीर्ति है। उनके जीते जी उनकी कोई भी एकल किताब प्रकाशित नहीं हुई।
हिन्दी में मुक्तिबोध अनोखा आश्चर्य है। इस आश्चर्य का उपनाम कैसे पड़ा यह भी विस्मित करता है। खिलजी शासनकाल में ऋग्वेदी कुलकर्णी ब्राह्मणों के किसी पूर्वज ने ‘मुग्धबोध’ या ‘मुक्तबोध’ नाम से कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा। कालांतर में उसी पर उनके वंश का नाम चल पड़ा। अंग्रेज़ी शासन काल में गजानन के परदादा वासुदेव महाराष्ट्र के जलगाँव से नौकरी छोड़कर मध्यप्रदेश के तत्कालीन ग्वालियर राज्य के श्योपुर आ गए। गोपालराव, जो कोतवाल थे, के इकलौते पुत्र माधवराव मुक्तिबोध थे। पिता के लगातार तबादलों से मुक्तिबोध की पढ़ाई बाधित होती रही। १९३० में वे मिडिल परीक्षा में फ़ेल हो गए थे। परीक्षा में फ़ेल होना मुक्तिबोध के जीवन की सबसे बड़ी घटना बनी। दूसरी बड़ी घटना उनकी पुस्तक ‘भारत: इतिहास और संस्कृति’ पर लगा प्रतिबंध था, जिसने उन्हें तोड़ दिया था।
हरिशंकर परसाई ने लिखा है- “जैसे ज़िंदगी में मुक्तिबोध ने किसी से लाभ के लिए समझौता नहीं किया, वैसे मृत्यु से भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। वे गहरे अंतर्द्वंद्व और तीव्र सामाजिक अनुभूति के कवि थे। उन्हें और तरह के क्लेश भी थे। भयंकर तनाव में वे जीते थे। पर फिर भी बेहद उदार, बेहद भावुक आदमी थे। उनके स्वभाव के कुछ विचित्र विरोधाभास थे। पैसे की तंगी में जीनेवाला यह आदमी पैसे को लात भी मारता था…”
मुक्तिबोध को लकवा मार गया था लेकिन उसके पहले उन्हें ‘परसिक्यूशन मेनिया’ सा हो गया था। उन्हें हवा में तलवारें दिखाई देतीं, रात को सपने में मोटी-मोटी छिपकलियाँ अपने ऊपर गिरती दिखतीं, वे पसीने-पसीने हो जाते। यदि कोई आदमी उनके पीछे आ रहा होता तो उन्हें लगता कि वह सीआईडी का आदमी है और जासूसी के इरादे से उनका पीछा कर रहा है। अंत के दिनों में उन्हें दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स में भर्ती कराया गया। दो-तीन महीने वे अचेत ही थे, उन्हें ट्यूबरकूलर मेनेंजाइटिस हो गया था। केवल ४७ वर्ष की अवस्था में गजानन माधव मुक्तिबोध इस दुनिया से कूच कर गए।
टाइमलाइन
१९३० में मिडिल परीक्षा फ़ेल।
१९३८ में होलकर कॉलेज इंदौर से बीए, उज्जैन के मॉर्डन स्कूल में अध्यापक।
१९३९ में पारिवारिक असहमति और विरोध के बावजूद शांता से प्रेम विवाह।
१९४० में शुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में अध्यापक, प्रभाकर माचवे से मुलाकात।
१९४१ में नेमीचंद से संपर्क और कविताओं का नया कलेवर।
१९४२ में स्कूल बंद, मित्र बिखर गए।
१९४३ सबसे पहले तार सप्तक में कविताएँ प्रकाशित।
१९४४ के अंत में इन्दौर में फ़ासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया, अध्यक्ष राहुल सांकृत्यायन।
१९४५ बनारस में त्रिलोचन शास्त्री के साथ हंस का संपादन।
- १९४८ में नागपुर में सूचना तथा प्रकाशन विभाग, आकाशवाणी और पत्र 'नया खून' में काम।
१९४६-४७ में जबलपुर के हितकारिणी स्कूल में अध्यापक, दैनिक जयहिंद में भी काम। समता द्वैमासिक में प्रमुख, फिर जबलपुर से नागपुर, ये सर्वश्रेष्ठ कविताओं और आर्थिक दृष्टि से जटिल दौर। नागपुर के संदर्भ ‘अंधेरे में’ कविता में दिखते हैं।
सन् १९५४ में एम ए।
१९५८ से मृत्यु तक राजनांदगाँव दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य, इसी दौर में ‘ब्रह्मराक्षस’, ‘ओरांट-उटांग’, ‘अंधेरे में’।
१९६२ में उनकी पुस्तक ‘भारत: इतिहास और संस्कृति’ पर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।
१९६४ में पक्षाघात
२००४ में मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बलदेव मिश्र की स्मृति में राजनांदगाँव में एक स्मारक का निर्माण।
रचनाएँ
चाँद का मुँह टेढ़ा है (कविता संग्रह), १९६४, भारतीय ज्ञानपीठ, २८ कविताएँ
काठ का सपना (कहानियों का संकलन), १९६७, भारतीय ज्ञानपीठ
सतह से उठता आदमी (कहानियों का संकलन), १९७१, भारतीय ज्ञानपीठ
नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध (निबंध), १९६४, विश्वभारती प्रकाशन
एक साहित्यिक की डायरी (निबंध), १९६४, भारतीय ज्ञानपीठ, १३ निबंध
विपात्र (उपन्यास), १९७०, भारतीय ज्ञानपीठ
नये साहित्य का सौन्दर्य-शास्त्र, १९७१, राधाकृष्ण प्रकाशन, १५ निबंध
कामायनी : एक पुनर्विचार, १९७३, साहित्य भारती
भूरी भूरी खाक धूल (कविता संग्रह), १९८०, राजकमल प्रकाशन, ४७ कविताएँ
मुक्तिबोध रचनावली (समग्र, ६ खंडों में), संपादक: नेमिचंद्र जैन, १९८०, राजकमल प्रकाशन
समीक्षा की समस्यायें, १९८२, राजकमल प्रकाशन
डबरे पर सूरज का बिंब, २००२, नेशनल बुक ट्रस्ट
भारत इतिहास और संस्कृति (आलोचनात्मक कृतियाँ)
स्वरांगी साने
कार्यक्षेत्र : कविता, कथा, अनुवाद,संचालन, स्तंभ लेखन, पत्रकारिता,अभिनय, नृत्य, साहित्य-संस्कृति-कला समीक्षा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वार्ता और काव्यपाठ
प्रकाशित कृति :
काव्य संग्रह “शहर की छोटी-सी छत पर” 2002, “वह हँसती बहुत है” 2019 में प्रकाशित।
http://kavitakosh.org/kk/otherapps/ebooks/?b=1g5HxLr55UYUvM7UdcmpUfSWFyWLXpNLQ
यू-ट्यूब पर swaraangi sane नाम से चैनल - #AMelodiousLyricalJourney




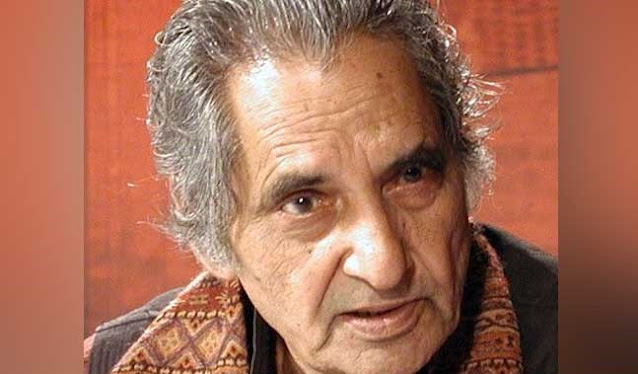
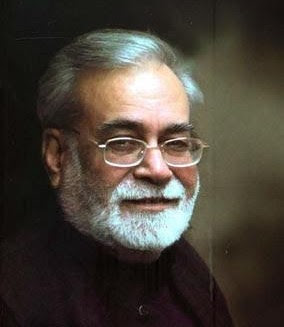











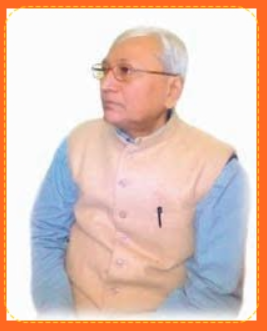

स्वरांगी जी को बहुत बहुत बधाई। मुक्तिबोध जैसे साहित्यकार की जीवन अनभूति एवं अंतर्द्वन्द को बखूबी लेख में उतारा है। बहुत बढ़िया लेख। हार्दिक बधाई।
ReplyDeleteमुक्तिबोध पर लिखने की छोटी-सी कोशिश की, आपको पसंद आई, जानकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका
Deleteस्वरांगी जी बहुत बढ़िया आलेख! मुझे याद है कि अंत समय में आपको यह आवंटित हुआ और आपने फुर्ती से यह लेख हमें दे दिया। शीघ्रता में भी गुणवत्ता बनाए रखमे का शुक्रिया!
ReplyDeleteशार्दुला जी मुक्तिबोध का नाम अपने आप में गुणवत्ता का पर्याय है, मैं अकिंचन उसका क्या श्रेय लूँ..आपको अच्छा लगा, प्रयास सफल मानती हूँ...बहुत धन्यवाद, स्नेह और अपनेपन के साथ...
Deleteस्वरांगी, बहुत बढ़िया आलेख, रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद।
ReplyDeleteआभारी हूँ सरोज जी आपकी
Deleteस्वरांगी जी,अद्भुत व रचनात्मक लेखन...पढ़कर आनंद आ गया👌🏻👌🏻👌🏻😊
ReplyDeleteबहुत बहुत आभार रश्मि शीतल जी..मुझे भी आपकी प्रतिक्रिया देख अच्छा लगा...
Delete@Swarangi Sane ऊबड़खाबड़ जीवन जीने वाले ऊबड़खाबड़ रचनाकार के जीवन के ऊबड़खाबड़ पहलुओं, कभी उतार कभी किंचित चढ़ाव, को बख़ूबी पेश किया है आपने। सुंदर और जानकारीपूर्ण आलेख के लिए बधाई और धन्यवाद।
ReplyDeleteबहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी, कोशिश की है कि लिख पाऊँ...पुनश्च धन्यवाद के साथ
ReplyDeleteस्वरंगी जी आपने जिस तरह से मुक्तिबोध जी के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को अपने सहज शब्दों में समेटा है , उनकी हर कृति का एक अनोखा विश्लेषण किया है वह मन को बहुत भाया ।
ReplyDeleteबहुत बहुत आभारी हूँ सोमा जी आपकी...कोशिश की है बस,....
Deleteबहुत बहुत आभारी हूँ सोमा जी आपकी...कोशिश की है बस,....
ReplyDeleteमुक्तिबोध पर विवरणपूर्ण लिखना जितना दुष्कर है उसे उतनी ही आसानी से वर्णित करने के लिए आपका बहुत आभार स्वरांगी।
ReplyDeleteबहुत अच्छा आलेख, स्वरांगी जी। मुक्तिबोध जी के जीवन के बहुत सारे आयाम पता चले।
ReplyDeleteतस्वीर भी बहुत मनोहारी है।
ReplyDelete